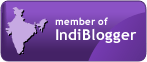भारतीय अपनी ही भाषाओं का तिरस्कार क्यों करते हैं?
मार्च 24, 2013
भारतीय (बेहतर होगा इंडियंस कहना ) अपनी ही भाषाओं का तिरस्कार क्यों करते हैं? इस सवाल का सर्वस्वीकार्य उत्तर शायद ही कोई दे सकता हो; हां अपनी-अपनी सोच के अनुसार लोग तमाम संभावनाओं की चर्चा कर सकते हैं । इस विषय में मेरे अपने कुछ विचार हैं किंतु उनका उल्लेख मैं इस आलेख में नहीं कर रहा हूं । इस समय मैं एक हालिया (7 मार्च) लेख की चर्चा करना चाहता हूं जो मुझे इकॉनॉमिस्ट-डाट-कॉम पर पढ़ने को मिला था । उसमें उल्लिखित कुछ बातें में यहां प्रस्तुत कर रहा हूं। उसमें कही गई जो बात मुझे खास लगी वह है “प्रायः सभी समाजों में लोग अपनी भाषाओं से अत्यंत लगाव रखते हैं। हिंदी एक अपवाद है।” अंग्रेजी में लिखित इस लेख का शीर्षक है “The keenest Wikipedians” (क्लिक करें) ।
10 लाख से अधिक विकीपीडिया लेख
लेख के अनुसार ‘विकीपीडिया’ विभिन्न भाषाओं में लिखित लेखों का भंडार बन चुका हैं, जिसमें उपलब्ध कई लेख अत्यंत उपयोगी पाए जाते हैं, पर सभी नहीं । विश्व की पांच भाषाओं में 10 लाख से भी अधिक लेख छप चुके हैं । ये भाषाएं हैं: अंग्रेजी (English), जर्मन (German), फ्रांसीसी (French), इतालवी (Italian), एवं डच (Dutch) ।
लेख में बताया गया है कि यूरोप के नेदरलैंड राष्ट्र के 100 प्रतिशत डचभाषी छात्र अंग्रेजी भी पढ़ते हैं, और प्रायः हर नागरिक फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकता है । ऐसा क्यों है कि अंग्रेजी जानने के बावजूद डच भाषा में इतने अधिक लेख छपते हैं, जब कि उस देश की जनसंख्या मात्र लगभग 1.7 करोड़ है ? लेखक के अनुसार इसका कारण मात्र यह है कि अन्य भाषाओं की अच्छीखासी जानकारी रखने के बावजूद लोग अपनी भाषाओं से अत्यंत लगाव रखते हैं और उसे ही इस्तेमाल करने की इच्छा रखते हैं ।
अपनी उस भाषा को जिसे लोग छोड़ने की नहीं सोचते उसे लेखक ने “अंडरवेयर लैंग्वेज” (Underwear Language) की संज्ञा दी है ।
1 से 10 लाख तक के लेख
अन्य भाषाओं, जिनके 1 लाख से अधिक लेख विकीपीडिया पर उपलब्ध हैं, में रूसी, अरबी एवं चीनी शामिल हैं । किंतु दिलचस्प तो यह है कि ऐसी भी कुछ भाषाएं हैं जो किसी देश की भाषा के रूप में स्थापित नहीं हैं, फिर भी उनमें छपे लेख 1 लाख से कम नहीं हैं, क्योंकि उन्हें बोलने वाले लोग है और वे उनका भरपूर प्रयोग करने का इरादा रखते हैं । इनमें शामिल हैं स्पेन में प्रचलित गैलिशियन (Galician), बास्क (Basque) तथा कैटलैन (Catalan) भाषाएं । ये स्पेन के उन बाशिंदों की भाषाएं हैं जो स्पेनी बोल सकते हैं और उसे इस्तेमाल भी करते हैं, फिर भी अपनी भाषाओं को प्रयोग में लेना पसंद करते हैं । लेख के अनुसार उक्त तथ्य इस बात का संकेत देता है कि लोग अपनी भाषाओं के प्रति विशेष लगाव रखते हैं ।
परंतु इससे अधिक चकित करने वाली बात तो यह है कि एस्परांटो (Esperanto, यूरोपीय भाषाओं में प्रचलित आम शब्दों पर आधारित एक कृत्रिम भाषा) में करीब 176,800 लेख विकीपीढिया में मिलते हैं । इसी प्रकार वोलापुक (Volapuk, एक अन्य कृत्रिम भाषा, जो लैटिन क्रियाओं को प्रयोग में लेते हुए मुख्यतः अंग्रेजी एवं कुछ सीमा तक जर्मन एवं फ्रांसीसी पर आधारित है) में 119,091 लेखों के छपे होने की बात कही गई है । यह भी जानकारी दी गई है कि इसके बोलने वाले कुछ गिने-चुने लोग ही हैं । फिर भी इतनी बड़ी संख्या में लेखों पर ताज्जुब ता होता ही है । ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने ‘ऑटोट्रांसलेशन’ के जरिये अन्य भाषाओं के लेख वोलापुक में डाल दिए हों ।
दिलचस्प यह है कि विकीपीढिया पर वोलापुक के लेखों की संख्या हिंदी में उपलब्ध लेखों से अधिक है । ऑटोट्रांसलेशन के माध्यम से तो हिंदी में भी लेख छप सकते हैं । फिर किसी ने ऐसा प्रयास क्यों नहीं किया होगा ?
हिंदी को लेकर लेखक की टिप्पणी सीधी-सी है: हिंदी कदाचित् ‘भाषाई लगाव के सिद्धांत’ का एक अपवाद है । अर्थात् हिंदीभाषी स्वयं अपनी भाषा से लगाव नहीं रखते और अंगरेजी लेखों का ही अध्ययन करते हैं । जब आपकी अपनी भाषा में रुचि ही न हो तो उसमें लेख लिखने की जहमत क्या उठाएंगे? यह स्थिति तब है जब हिंदी में लिखित रचनाओं की कोई कमी नहीं और इसके बोलने वाले लोगों की संख्या दशियों करोड़ों में है – किसी भी यूरोपीय भाषा के बोलने वालों से अधिक ।
1 लाख से कम लेख
लेखक ने इस पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि अलेमानिक (Alemannic) पीडमोंटीज (Piedmontese) जावानीज (Javanese) में भी लेखों की संख्या (क्रमशः 13,708, 59,303, तथा 43,122) निराशाप्रद है, जब की इनके भाषाभाषियों की संख्या करोड़ों में है । स्पष्ट है कि संबंधित लोग उन अन्य भाषाओं में लेख पढ़ते हैं जिन्हें वे जानते हैं ।
आगे यह भी जानकारी दी गई है कि हावजू (Zhosa) में मात्र 146 लेख ही उपलब्ध हैं । इस भाषा के जानने वालों की संख्या करीब 80 लाख बताई गई है और यह भी कि नेल्सन मंडेला की मातृभाषा है । अपनी भाषाओं के प्रति उदासीनता काफी व्यापक है, और यह उसका एक उदाहरण है ।
विकीपीडिया लेखों के भाषाई आधार पर विभाजन के अध्ययन में एक भाषा हेरेरो (Herero, कुछ अफ्रिकी देशों में बोली जाने वाली भाषाओं में से एक) का भी जिक्र है, जिसमें एक भी लेख शामिल नहीं है, यद्यपि उसका होमपेज बना हुआ है ।
भाषाई गहराई
लेखक ने भाषाई गहराई (Depth of Language) को भी परिभाषित किया है । अध्ययनकर्ता के अनुसार अहमियत केवल इस बात की नहीं होती है कि कितने लेख अमुक भाषा में लिखित पाए जाते हैं । यह बात भी अहमियत रखती है कि उन लेखों को कितना संपादित किया जाता है, जो लोगों की सक्रिय दिलचस्पी का द्योतक हैं । भाषाई गहराई को दोनों (संख्या एवं गहराई) के अनुपात के तौर पर परिभाषित किया गया है । उम्मीद के अनुरूप 42 लाख लेखों के साथ अंगरेजी अन्य भाषाओं के बहुत आगे पाई गई है । रोचक तथ्य यह भी है कम लेखों के बावजूद हिब्रू, अरबी, फारसी, तथा तुर्की इस गहराई के मामले में जर्मन एवं इतालवी के आगे हैं । हिंदी कहां पर है इसका जिक्र नहीं किया गया है । चीनी भाषा की चर्चा भी कहीं नहीं दिखी ।
बहरहाल इस दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य पर अपने देशवासियों को विचार करना चाहिए कि जिस भाषा को राजभाषा का तमगा पहनाया गया है और जो अनेकों जनों की मातृभाषा है, उसी के बोलने वाले उसे इतनी हिकारत की निगाह से क्यों देखते हैं । क्या यह हमारी मानसिक ग़ुलामी का द्योतक है, यानी कि देश राजनैतिक तौर पर तो आज़ाद हो गया लेकिन दिमागी तौर पर नहीं । हाल में संघ लोकसेवा आयोग (UPSC) की परीक्षाओं में अंगरेजी का कद बढ़ाने और देशी भाषाओं को हासिये पर डालने का निर्णय इसी मानसिकता का संकेतक है । (फ़िलहाल वह निर्णय टल गया है ।) – योगेन्द्र जोशी
‘इंडिया दैट इज भारत’ क्या वास्तव में स्वतंत्र हो पाया है ? यह ऐसा सवाल है जिसका उत्तर मैं ‘नहीं’ में पाता हूं । मेरी दृष्टि में अंग्रेजों द्वारा भारतीय राजनेताओं के हाथों में सत्ता का राजनैतिक हस्तांतरण कर दिये जाने की व्याख्या पूर्ण स्वतंत्रता के रूप में नहीं की जा सकती है । स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत तत्कालीन राजनेताओं ने आशा की थी कि राजनैतिक स्वतंत्रता के बाद कालांतर में यह देश अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत से भी मुक्त हो जाएगा । परंतु ऐसा हो नहीं पाया ।
आज स्थिति यह है कि अंग्रेजी एवं अंग्रेजियत ने इस देश को पूरी तरह कब्जे में ले लिया है । मैं यहां पर अंग्रेजी के हिंदी पर पड़ रहे कुप्रभाव की बात कर रहा हूं । यों तो अंग्रेजी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकृत कर डाला है, किंतु मेरी बात हिंदी तक सीमित रहेगी । इस देश में महानगरों में संपन्न, अंग्रेजी-शिक्षित एक ऐसा वर्ग उभर रहा है, जो स्वयं को हिंदीभाषी बताता है, किंतु जिसे हिंदी में वास्तविक रुचि रह नहीं गयी है । यह ऐसा वर्ग है जो हिंदी को अपनी मातृभाषा घोषित करता है, किंतु साफ-सुथरी हिंदी न तो बोल सकता है और न लिख सकता है । वह ऐसी भाषा बोलने लगा है जो हरगिज हिंदी नहीं कही जा सकती है । इस भाषा को हिंग्लिश कहना भी उचित नहीं होगा । इसे मैं ‘मेट्रोहिंदी’ अथवा ‘एचईमिक्स’ कहना चाहूंगा ।
मेट्रोहिंदी
इसका ‘मेट्रोहिंदी’ नामकरण मैं इसलिए करता हूं, क्योंकि यह मुख्यतया महानगरों, ‘मेट्रोसिटीज्’, के शिक्षित एवं संपन्न लोगों द्वारा प्रयोग में ली जा रही है । इसका प्रभावक्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है । इसकी पहुंच छोटे शहरों से होते हुए कस्बों-गांवों तक के शिक्षित लोगों तक हो रही है । इस भाषा की खासियत यह है कि इसकी शब्दसंपदा में कितने अंग्रेजी शब्दों को शामिल किया जाएगा इस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है । अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग वक्ता के अंग्रेजी ज्ञान एवं उसकी सुविधा पर निर्भर करता है । यहां तक कि उसका व्याकरणीय ढांचा भी आवश्यकतानुसार तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है और अंग्रेजी व्याकरण के अनुरूप ढाला जा सकता है । इस भाषा में अंग्रेजी के पदबंध (फ्रेज), वाक्यांश, एवं कभी-कभी पूरे वाक्य स्वीकार्य रहते हैं । इसी अर्थ में मेट्रोहिंदी को मैं विकल्पतः ‘एचईमिक्स’ भी कहता हूं, एचईमिक्स अर्थात् ‘हिंदी-इंग्लिश-मिक्स्चर’ । मैं इस भाषा को हिंग्लिश नहीं मानता, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के शब्दों की ही बहुतायत नहीं है, बल्कि उसके आगे बहुत कुछ – जी हां बहुत कुछ – और भी है ।
मेट्रोहिंदी अभी औपचारिक रूप से स्थापित भाषा नहीं है । इसका अस्तित्व तो है, किंतु ऐसा लगता है कि अभी भाषाविदों ने इसका अध्ययन पारंपरिक हिंदी से भिन्न स्वयं में एक नई भाषा के तौर पर करने का प्रयास नहीं किया है । कदाचित् सभी भारतीय इसे हिंदी की ही आधुनिक बोली मानकर चलते हों । लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता । हिंदी से मिलती-जुलती होने के बावजूद उर्दू एक अलग भाषा कही जाती है । ठीक वैसे ही मेट्रोहिंदी को हिंदी से मिलती-जुलती लेकिन उससे अलहदा भाषा माना जाना चाहिए ।
एक बानगी
मेट्रोहिंदी की क्या खासियत है और इसके उपयोक्ता कौन हैं इन पर अपना मत व्यक्त करने से पहले में एक बानगी पेश करता हूं । आजकल ब्राजील के दूसरे सबसे बड़े शहर रिओ द जनेरो (Rio de Janeiro) में जलवायु परिवर्तन (Climate Change) पर विभिन्न राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की बैठक चल रही है । निम्नलिखित अनुच्छेद मैंने New Scientist पत्रिका के वेबसाइट पर उक्त बैठक से संबंधित रपट (18 June 2012) से उद्धृत किया है । अंग्रेजी में इसका मूल पाठ यों है:
“The Earth Summit in this week is not looking promising. The conference will be devoid of the world leaders who attended its predecessor, 20 years ago. And there are no headline-grabbing treaties to sign. Its final declaration will not be binding to anyone. The main outcome will probably be to launch a set of “sustainable development goals” on issues like protecting forests, fisheries and water supplies.”
हिंदी संवाददाता, विषय-समीक्षक, अथवा प्रशासनिक प्रवक्ता, जो अंग्रेजी में ही कार्य करने का आदी हो चुका हो और जिसे साफसुथरी हिंदी के प्रयोग का अभ्यास ही न रह गया हो, उक्त अनुच्छेद को अंग्रेजीकृत ‘हिंदी’ (अर्थात् मेट्रोहिंदी) में कुछ यों प्रस्तुत करेगा:
“रिओ द जनेरो में चल रही इस वीक की अर्थ समिट प्रोमिसिंग नहीं लग रही है । इस कॉंफरेंस में उन वर्ल्ड लीडर्स की कमी रहेगी जिन्होंने 20 साल पहले इसका प्रिडिसेसर अटेंड किया था । और इसमें हेडलाइनलाइन-ग्रैबिंग ट्रीटीज साइन करने के लिए नहीं हैं । इसका फाइनल डिक्लेरेशन किसी के लिए बाइंडिंग नहीं होगा । संभवतः इसका मेन आउटकम फॉरेस्ट, फिशरीज्, एंड वाटर सप्लाइज् के प्रोटेक्शन के इश्यूज् पर “सस्टेनेबल् डिवेलपमेंट गोल्ज” पेश करना रहेगा ।”
(ध्यान दें कि अपने निजी टीवी चैनलों पर हिंदी समाचार प्रस्तुति कुछ ऐसी ही रहती है!)
यह हिंदी नहीं है । उसमें मौजूद अंग्रेजी शब्दों की अवांछित भरमार इसे उस व्यक्ति की समझ से बाहर कर देती है, जिसका अंग्रेजी ज्ञान पर्याप्त न हो । जो लोग अंग्रेजी के उक्त प्रकार के शब्द निर्लज्जता के साथ प्रयोग में लेते हैं उन्हें इस बात की परवाह नहीं रहती है कि ऐसी वैचारिक प्रस्तुति आम हिंदीभाषी की समझ से परे होगी । वह यह मानता है हर हिंदीभाषी को अंग्रेजी ज्ञान तो होना ही चाहिए । इसके विपरीत वह यह हरगिज नहीं मानता कि जब वह हिंदी बोलता है तब वह वास्तव में हिंदी ही बोले । अन्यथा हिंदी बोलने का नाटक न करके अंग्रेजी में बोले ।
जैसे अंग्रेजी समाचारों में आप हिंदी शब्दों को मनमरजी से नहीं ठूंसते, वैसे ही हिंदी समाचारों में अंग्रेजी शब्द महज इसलिए नहीं ठूंसे जा सकते हैं क्योंकि आपको हिंदी शब्द नहीं सूझते । इस तर्क को ध्यान में रखते हुए उक्त अनुच्छेद साफसुथरी हिंदी में कुछ ऐसे प्रस्तुत होना चाहिए:
“रिओ द जनेरो में चल रही इस सप्ताह का पृथ्वी सम्मेलन सफल होते नहीं लग रहा है । इस सम्मेलन में विश्व के उन नेताओं की कमी रहेगी, जिन्होंने 20 साल पहले इसके पूर्ववर्ती में भाग लिया था । और इसमें हस्ताक्षर करने के लिए समाचार-शीर्षक बनने योग्य समझौते भी नहीं हैं । इसका अंतिम घोषणापत्र किसी के लिए बाध्य नहीं होगा । संभवतः इसका मुख्य प्रतिफल वन, मत्स्यक्षेत्र, एवं जलापूर्ति के संरक्षण के मुद्दों पर “विकास के चिरस्थाई लक्ष्य” पेश करना रहेगा ।” (यह मेरा अनुवाद है; कदाचित् इससे बेहतर अनुवाद संभव हो ।)
मेट्रोहिंदी की वे खासियतें जो इसे आम हिंदी से अलहदा बनाती हैं, और वे कौन हैं जो इसे प्रयोग में ले रहे हैं इन बातों की चर्चा इस चिट्ठे की अगली प्रविष्टि में किया जाएगा । – योगेन्द्र जोशी
हिंदी दिवस (14 सितंबर) – कल एक पुरानी पोथी की तरह कपड़े में लपेटकर …
सितम्बर 14, 2011
आज (14 सितंबर) हिंदी दिवस है । इस अवसर पर प्रथमतः देशवासियों, विशेषतः हिंदीप्रेमियों, के प्रति शुभेच्छा संदेश देना चाहता हूं ।
असल में आज हिंदी का जन्मदिन है बतौर राजभाषा के । अन्यथ हिंदी भाषा तो सदियों से अस्तित्व में है । आज के दिन 61 साल पहले उसे राजभाषा होने का गौरव मिलाए और इसी अर्थ उसका जन्मदिन है । उसे वैधानिक सम्मान तो मिला, किंतु ‘इंडियन’ प्रशासनिक तंत्र से वह सम्मान नहीं मिला जो राजभाषा घोषित होने पर मिलना चाहिए था । यह कमोबेश वहीं की वहीं है । और रोजमर्रा के जीवन में उसका जितना भी प्रयोग देखने को मिल रहा है, वह राजभाषा के नाते कम है और जनभाषा होने के कारण अधिक है ।
आज हिंदी का सही माने में जन्मदिन है । जैसे जन्मदिन पर उत्सव का माहौल रहता है, संबंधित व्यक्ति को शुभकामनाएं दी जाती हैं, उसके दीर्घायुष्य की कामना की जाती है, इत्यादि, उसी भांति आज हिंदी का गुणगान किया जाता है, उसके पक्ष में बहुत कुछ कहा जाता हैं । उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है अगले जन्मदिन तक । जैसे जन्मदिन रोज नहीं मनाया जाता है, उसी प्रकार हिंदी की बात रोज नहीं की जाती है । उसकी शेष चिंता अगले हिंदी दिवस तक भुला दी जाती है । लोग रोज की तरह ‘जन्मदिन’ मनाकर सामान्य जीवनचर्या पर लौट आते हैं ।
आज के बुद्धिजीवियों के द्वारा वार्तापत्रों/पत्रिकाओं में हिंदी को लेकर भांति-भांति के उद्गार व्यक्त किए जाते हैं । मेरे पास प्रातःकाल हिंदी के दो दैनिक समाचारपत्र आते हैं, दैनिक हिन्दुस्तान एवं अमर उजाला । मैंने हिंदी से संबंधित उनमें क्या छपा है, इसे देखना/खोजना आरंभ किया । आज के हिन्दुस्तान समाचारपत्र के संपादकीय पृष्ठ पर छपे एक व्यंगलेख ने मेरा ध्यान सर्वाधिक खींचा । उसमें लिखा थाः
“… आज पूज रहे हैं, दिवस मना रहे हैं । कल एक पुरानी पोथी की तरह कपड़े में लपेटकर ऊंचे पर रख देंगे । …”
यह वाक्य कटु वास्तविकता का बखान करता है, जैसा में पहले ही कह चुका हूं । इसी पर आधारित मैंने इस लेख का भी शीर्षक चुना है ।
इसी पृष्ठ पर 75 साल पहले के समाचार का भी जिक्र देखने को मिला, जिसमें तत्कालीन राजकीय निर्णय का उल्लेख थाः “… सिक्कों पर केवल अंग्रेजी (रोमन) एवं उर्दू (अरबी) लिपि ही रहेंगी ।…” अर्थात् देवनागरी लिपि की तब कोई मान्यता ही नहीं थी ।
उक्त समाचारपत्र के अन्य पृष्ठ पर “हिंदी के आईने में कैसी दिखती है हमारी युवा पीढ़ी” नाम का एक लेख भी पढ़ने को मिला । इसमें महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के छात्रों का हिंदी संबंधी ज्ञान की चर्चा की गयी है । ‘किडनी’ जैसे अंग्रेजी शब्दों, ‘पानी-पानी होना’ जैसे मुहावरों, ‘हजारी प्रसाद द्विवेदी’ जैसे लेखकों आदि के बारे में छात्रों से जानकारी ली गयी थी । कइयों के उत्तर भाषाई स्थिति की भयावहता का दर्शन कराते हैं । उनका ज्ञान नैराश्यजनक है ।
इस समाचारपत्र में एक स्थान पर सिनेमा एवं टीवी क्षेत्र की कुछ हस्तियों के हिंदी संबंधी विचारों का भी उल्लेख किया गया है । देखिए क्या कहा उन लोगों ने
“आवाम से बात हिंदी में होगी” – महमूद फारूकी
“मैं ख्वाब देखूं तो हिंदी में, मैं ख्याल यदि सोचूं तो हिंदी में” – कैलाश खेर
“हिंदी को प्राथमिक और अंग्रेजी को गौण बनाकर चलें” – रिजवान सिद्दीकी
“मैं उसकी काउंसिलिंग करना चाहूंगा जो कहता है हिंदी में करियर नहीं” – खुराफाती नितिन
“हिंदी बढ़ा देती है आपकी पहुंच” – अद्वैत काला
“बिना हिंदी सीखे नहीं चला काम” – कैटरीना कैफ
“हिंदी ने ही मुझे बनाया” – शाहरूख खान
“टीवी में हिंदीभाषियों के लिए मौके ही मौके” – साक्षी तंवर
“हिंदी तरक्की की भाषा है” – प्रकाश झा
“मेरे सपनों की भाषा है हिंदी” – आशुतोष राणा
“अनुवाद से लेकर अभिनय, सबमें हिंदी ने दिया सहारा” – सुशांत सिंह
इन लोगों के उद्गार उनकी वास्तविक सोच का ज्ञान कराती हैं, या ये महज औपचारिकता में बोले गये शब्द हैं यह जान पाना मेरे लिए संभव नहीं । कम ही विश्वास होता है कि वे सब सच बोल रहे होंगे । फिर भी आशुतोष राणा एवं एक-दो अन्य जनों के बारे में सच होगा यह मानता हूं ।
मेरे दूसरे समाचारपत्र अमर उजाला में काफी कम पाठ्य सामग्री मुझे पढ़ने को मिली । उसमें कही गयी एक बात अवश्य आशाप्रद और जमीनी वास्तविकता से जुड़ी लगती है मुझे । लेखक ने श्री अन्ना के हालिया आंदोलन का जिक्र करते हुए इस बात को रेखाकिंत किया है कि अंग्रेजी की जितनी भी वकालत ‘इंडियन’ बुद्धिजीवी करें, हकीकत यह है कि आम आदमी को वांछित संदेश तभी पहुंचता है जब बात जनसामान्य की जुबान में कही जाती है । हिंदी ऐसी सर्वाधिक बोली/समझी जाने वाली जुबान है । यह वह भाषा है जो देश के अधिकांश क्षेत्रों में समझी जाती है । अन्य स्थानों पर भी समझने वाले मिल जाएंगे और उनकी संख्या बढ़ रही है । गैरहिंदीभाषी क्षेत्रों के कई लोग हिंदी कुछ हद तक इसलिए भी समझ लेते हैं कि उनकी अपनी भाषा का हिंदी से काफी हद तक साम्य है, भले ही वे बोल न सकें । आसाम, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र ऐसे ही क्षेत्र हैं । अंग्रेजी के संबोधनों और लेखों के पाठक आम आदमी नहीं होते हैं, अतः बातें सीमित दायरे में और आम आदमी की पहुंच से बाहर रह जाती हैं । अन्ना जी का अंग्रेजी ज्ञान नहीं के बराबर है, फिर भी मराठी पुट के साथ हिंदी में कही गयी उनकी बातें जनमानस तकपहुंच सकीं । इस तथ्य को हमारे राजनेता बखूबी जानते हैं । तभी तो वे चुनावी भाषण हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में देते हैं, शायद ही कभी अंग्रेजी में । (एक सवालः अन्ना के बदले अण्णा क्यों नहीं लिखते हिंदी पत्रकार ? मराठी में तो उसकी वर्तनी यही है !)
अमर उजाला के संपादकीय पृष्ठ पर हिंदी के राजभाषा बनाए जाने और 1950 की 14 सितंबर की तारीख पर उसके सांविधानिक मान्यता पाने के बारे में भी संक्षिप्त लेख छपा है । अन्य लेख में नौकरशाही पर उनकी अंग्रेजी-भक्ति पर कटाक्ष भी है । श्री मणिशंकर अय्यर का दृष्टांत देते हुए उनकी अंग्रेजीपरस्त सोच की चर्चा की है । दरअसल इस देश की नौकरशाही ही है जो हिंदी को दस्तावेजी भाषा बनने में अड़ंगा लगाती आ रही है । निराशा तो इस बात को देखकर होती है कि जो युवक हिंदी माध्यम से प्रशासनिक सेवाओं में नियुक्ति पाते हैं वे भी हीन भावना से ग्रस्त होकर शनैःशनैः अंग्रेजियत के रंग में रंग जाते हैं । वे क्या कभी स्वयं को एवं देशवासियों को इस भ्रम से मुक्ति दिला पाएंगे कि विश्व में सर्वत्र अंग्रेजी ही चलती है । इस देश में जैसा अंग्रेजी-मोह देखने को मिलता है वैसा किसी भी प्रमुख देश में देखने को नहीं मिलता है । भ्रमित नौकरशाही को अंग्रेजी की व्यापकता के अज्ञान से मुक्ति मिले यही मेरी प्रार्थना है ।
मुझे दो-चार दिन पहले एक ई-मेल से इंटरनेट लिंक मिला था, जो एक लेख पर मुझे ले गया जिसमें अंग्रेजी से इतर विश्व की उन भाषाओं का जिक्र है जिन्हें व्यावसायिक कार्य में लिया जाता है । भारतीय भाषाओं में से कोई भी दी गयी सूची में शामिल नहीं है । इस बारे दो-चार शब्द लिखने का मेरा विचार था, लेकिन अब उस पर अगले लेख में ही कुछ बोलूंगा । -योगेन्द्र जोशी
PIDGIN (पिजिन), CREOLE (क्रिओल) एवं Hinglish (हिंग्लिश)
सितम्बर 5, 2010
PIDGIN – A simple form of a language with elements taken from the local languages used for communication between people not sharing a common language. Origin: Chinese alteration for business.
CREOLE – 1 a person of mixed European and Black descent. 2 a descendent of European settlers in the Caribbians or Central or South America. 3 a descendent of French settlers in the south of US. 4 a language formed with the combination of a European Language and an African Language.
पिजिन
‘पिजिन’ एवं ‘क्रिओल’ की ये परिभाषाएं कॉम्पैक्ट ऑक्सफर्ड रेफरेंस डिक्शनरी (Compact Oxford Reference Dictionary) से ली गयी हैं । अंतरजाल पर खोजने पर आपको इन शब्दों की व्याख्या अलग-अलग प्रकार से मिलेगी, लेकिन सभी का सार एक ही रहता है । देखने-पढ़ने के लिए संदर्भों की संख्या की कोई कमी नहीं हैं । मैंने निम्नलिखित को अधिक ध्यान से देखा था:
http://privatewww.essex.ac.uk/~patrickp/Courses/CreolesIntro.html
http://humanities.uchicago.edu/faculty/mufwene/pidginCreoleLanguage.html
http://logos.uoregon.edu/explore/socioling/pidgin.html
पिजिन (Pidgin) वस्तुतः एक मिश्रित बोली है । इसे भाषा कहना उचित नहीं होगा । जब ऐसे व्यक्ति-समूह परस्पर मिलते हैं जो एक-दूसरे की भाषा/बोली न जानते हों, किंतु उन्हें परस्पर व्यावसायिक/व्यापारिक संबंध स्थापित करने हों, तब कामचलाऊ बोली का जन्म होता है । दो या अधिक भाषाओं के शब्दों की खिचड़ी बोली जिससे परस्पर का कार्यव्यापार चल जाए वह पिजिन कहलाती है । बताया जाता है कि ‘पिजिन’ शब्द अंग्रेजी शब्द बिजनेस (business) का चीनी भाषा में रूपांतर है । शब्द की व्युत्पत्ति का खास इतिहास नहीं है । कहा जाता है कि पिजिन शब्द 1807 से प्रचलन में है ।
पिजिन बोलियों के इतिहास का यूरोपियों द्वारा अमेरिकी द्वीपों में उपनिवेश स्थापित करने से घनिष्ठ संबंध रहा है । स्थानीय जनसमुदायों के साथ काम भर का संपर्क स्थापित करने अथवा उनकी श्रमशक्ति का उपयोग करने के लिए ऐसी टूटी-फूटी बोली का प्रचलन हुआ । इतना ही नहीं, कई क्षेत्रों में कृषि एवं अन्य कार्यों के लिए वे लोग अपने साथ अफ्रिकी ‘गुलामों’ को भी ले गये । उनके साथ संवाद के लिए भी ऐसी बोली प्रचलन में आई । इन अवसरों पर ‘सभ्य’ कहे जाने वाले और समुन्नत भाषाओं के धनी यूरोपियों की उन श्रमिकों या ‘गुलामों’ की अपेक्षया अविकसित भाषा सीखने में स्वाभाविक तौर पर कोई दिलचस्पी नहीं रही होगी । दूसरी तरफ श्रमिकों/‘गुलामों’ में भी इतनी क्षमता कदाचित् नहीं रही होगी कि वे ‘मालिकों’ की भाषा को सरलता से अपना लें । दोनों प्रकार के समुदायों का परस्पर संपर्क केवल जरूरी कार्यव्यापार तक सीमित था जिसके लिए पिजिन से काम लेना पर्याप्त था । श्रमिक/‘गुलाम’ जब स्वयं ही अलग-अलग क्षेत्रों के मूल बाशिंदे होते थे, तब वे भी आपस में पिजिन का सहारा लेते थ और उस बोली में दो से अधिक भाषाओं/बोलियों के शब्द शामिल हो जाते थे । इन मिश्रित बोलियों को संबंधित भाषाओं के नाम से पुकारा जाने लगा, यथा पापुआ न्यू गिनी पिजिन जर्मन (Papua New Guinea Pidgin German ), कैमरून पिजिन इंग्लिश (English based Cameroon Pidgin) आदि ।
पिजिन बोली का कोई सुनिश्चित व्याकारणीय स्वरूप नहीं रहता । इसकी शब्दसंपदा बेहद कम और कामचलाऊ रहती है, जिसमें संबंधित भाषाओं के शब्द रहते हैं । आम तौर यूरोनीय भाषा के शब्द अधिक रहते हैं जब कि उनका उच्चारण, वाक्य में क्रम, आदि स्थानीय बोली पर अधिक आधारित रहते हैं । प्रमुख भाषा को उपरिस्तरीय (Superstrate) एवं गौण को अधोस्तरीय (Substrate) कहा जाता है । पिजिन का एक उदाहरण (उपर्युक्त किसी जालस्थल से लिया गया कैमरून पिजिन इंग्लिश) देखिए:
dis smol swain i bin go fo maket (दिस स्मोल स्वैन इ बिन गो फो माकेट) = this little pig went to market
पिजिन एवं क्रिओल (आगे देखें) का अध्ययन अपने देश में शायद नहीं होता है, किंतु यूरोप एवं अमेरिका के कुछ शिक्षण संस्थाओं के भाषा विभागों में इनके बारे में पढ़ाया जाता है (जैसे एसेक्स वि0वि0, ब्रिटेन, एवं शिकागो वि0वि0, अमेरिका) ।
क्रिओल
पिजिन की भांति क्रिओल भी एक मिश्रित या वर्णसंकर (Hybrid) बोली है । यों समझा जा सकता है कि जब पिजिन समय के साथ परिष्कृत होकर स्थायित्व धारण कर लेती है तो वही क्रिओल कहलाने लगती है । यह माना जाता है कि अफ्रिकी, अमेरिकी देशों के अपेक्षया पिछड़े जनसमुदायों की भाषा पर यूरोपीय भाषाओं के अत्यधिक प्रभाव से क्रिओलों का जन्म हुआ है । आरंभ में वे जनसमुदाय अपनी मूल भाषा का ही प्रयोग करते रहे, किंतु व्यापारिक/व्यावसायिक संपर्क के कारण पिजिन का प्रयोग भी साथ-साथ चलता रहा । कालांतर में आने वाली पीढ़ियां पिजिन के आदी होते चले गये । इस प्रक्रिया के फलस्वरूप ऐसी भाषा व्यवहार में आई जिसने एक स्पष्ट व्याकरणीय ढांचा इख्तियार कर लिया और जिसका एक अच्छा-खासा शब्दसंग्रह भी तैयार हो गया । संबंधित मूल भाषाओं के नामों पर आधारित क्रिओल संबोधन से यह भाषा पुकारी जाने लगी ओर उन लोगों की आम भाषा ही बन गयी ।
विषय के जानकारों के अनुसार क्रिओलों की शब्दसंपदा मुख्यतः बाहरी (यूरोपीय) भाषा पर आधारित रहती है जब कि वाक्यविन्यास स्थानीय भाषा पर । स्थानीयता शब्दों के स्वरूप एवं अर्थ को प्रभावित करती है । अंग्रेजी-आधारित जमैकी पिजिन में शब्द रचना का एक दृष्टांत देखें: हैन-मिगल् = हथेली (Han-migl = hand+middle = palm) ।
पापुआ न्यू गिनी में अंग्रेजी और स्थानीय भाषा से प्राप्त टोक पिसिन (Toke Pisin = Talk Pidgin?) नाम की क्रिओल राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है और देश की ‘असेम्बली’ और रेडियो प्रसारण में प्रयुक्त होती है । इसका एक वाक्य यह है:
“Sapos yu kaikai planti pinat, bai yu kamap strong olsem phantom.”
(सापोस यू काइकाइ प्लान्टी पीनाट, बाइ यू कमअप स्ट्रॉंग ओल्सम फैंटम ।)
“If you eat plenty of peanuts, you will come up strong like the phantom.”
अमेरिका में लूसियाना क्रिओल प्रचलन में है, जो फ्रांसीसी एवं अफ्रिकन भाषाओं पर आधारित है । अन्य कुछ क्रिओल भाषाएं ये हैं: Haitian, Mauritian, and Seychellois (French based); Jamaican, Guyanese, and Hawaiian Creole (English based); Cape Verdian Criolou (Portuguese based) and Papiamentu in the Netherlands Antilles (Portuguese based, Spanish influenced) |
हिंग्लिश
इस आलेख में मेरा मुख्य उद्येश्य है हिंग्लिश पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करना । पिजिन एवं क्रिओल की संक्षिप्त परिचयात्मक चर्चा के पीछे प्रयोजन यह रहा है कि इनके सापेक्ष हिंग्लिश को तौला जा सके । मेरे विचार में स्वतंत्र इंडिया दैट इज भारत (ह्विच इट इज नॉट!) की एक बड़ी, किंतु नकारात्मक, उपलब्धि रही है हिंग्लिश की प्रतिष्ठापना । हिंग्लिश हिंदी एवं अंग्रेजी के घालमेल से बनी एक वर्णसंकर भाषा है, जिसके बीज तो अंग्रेजी राज में पड़ चुके थे, लेकिन जिसका विकास एवं अधिकाधिक प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही हुआ ।
मैं यह निश्चित नहीं कर पा रहा हूं कि हिंग्लिश को पिजिन कहा जाए या क्रिओल । पिजिनों/क्रिओलों के प्रचलन में आने की जिन परिस्थितियों की बात कही गयी है वे अवश्य ही हिंग्लिश पर लागू नहीं होती हैं । अंग्रेजी राज से पहले से जो भी भाषाएं इस भूभाग में प्रचलित रही हैं वे उच्च दर्जे की रही हैं और अभिव्यक्ति के स्तर पर वे यूरोपीय भाषाओं से कमतर नहीं मानी जा सकती हैं । यहां के लोग आवश्यकतानुसार अंग्रेजी तथा अन्य भाषाएं सीखने में समर्थ थे और उन्होंने उन्हें सीखा भी । फिरंगियों के समय में ऐसी परिस्थितियां नहीं थीं कि किसी पिजिन/क्रिओल की जरूरत रही हो । उनका राज यही के लोग चला रहे थे, जो अंग्रेजी के साथ एक (मातृभाषा) या अधिक भाषाएं बोल/लिख सकते थे । तब फिर हिंग्लिश की जरूरत क्यों पड़ी ? अंग्रेजी शासन चलाने में योगदान दे रहे वे लोग इतने सक्षम रहे कि वे इन भाषाओं को साफ-सुथरे रूप में प्रयोग में ले सकते थे । तो फिर हिंग्लिश तथा उसी तर्ज पर ‘बांग्लिश’, ‘कन्नलिश’, ‘गुजलिश’ जैसी वर्णसंकर भाषाओं का प्रचलन तेजी से क्यों बढ़ा ?
हिंग्लिश की बात तो मैंने कर दी पर यह स्पष्ट नहीं किया कि यह आखिर है क्या ? यह आज के हिंदुस्तान के शहरी पढ़े-लिखे लोगों के बीच पूर्णतः प्रचलित हो चुकी एक भाषा है जिसका व्याकरणीय ढांचा तो हिंदी का है, किंतु शब्दसंग्रह कमोबेश अंग्रेजी का है । यह उन लोगों की देन है जो चमड़ी के रंग से तो हिंदुस्तानी हैं, लेकिन जो दिल से अंग्रेज बन चुके हैं । ये वे लोग हैं जो भारतीय भाषाओं को केवल मजबूरी में ही प्रयोग में लेना चाहते हैं, जिन्हें मूल/मातृ- भाषा की शब्दसंपदा समृद्ध करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जिनके मुख से मौके पर हिंदी का उचित शब्द नहीं निकल सकता है । हिंदी में अंग्रेजी के शब्दों को जहां तबियत हुई वहां ठूंस देने में उन्हें कोई हिचक नहीं होती है । उन्हें इस बात पर कोई कोफ्त अथवा लज्जा अनुभव नहीं होती कि वे अपनी ‘तथाकथित’ मातृभाषा में भी ठीक से नहीं बोल सकते, विचारों को व्यक्त नहीं कर सकते । वे इस बात की तनिक भी चिंता नहीं करते हैं कि जिससे वे बात कर रहे हैं उसके भेजे में उनकी यह नयी भाषा घुस भी पा रही कि नहीं । हिंदीभाषियों का बृहत्तर जनसमुदाय उनकी भाषा वस्तुतः नहीं समझ सकता । हिंग्लिश में व्यक्त इस कथन पर गौर करें:
“चीफ़-मिनिस्टर ने नैक्सलाइट्स को डायलॉग के लिए इंवाइट किया है । लेकिन नैक्सलाइट्स अन्कंडिशनल मीटिंग के लिए तैयार नहीं हैं । उनका कहना है कि सरकार कांबिग आपरेशन बंद करे और उन्हें सेफ पैसेज दे तो वे निगोशिएशन टेबल पर आ सकते हैं ।”
इस कथन को सड़क पर का आम आदमी (man on the street) क्या वास्तव में समझ सकता है ? उसे मालूम है कि कांबिग क्या होती है और निगोशिएशन किसे कहते हैं, आदि ? जरा सोचें ।
इस देश में अंग्रेजीपरस्त एक ऐसा वर्ग उभरा है जिस पर ‘सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है’ की कहावत चरितार्थ होती है । निःसंदेह उसके पास अंग्रेजी शब्दों का अपार शब्दभंडार है, किंतु आम हिंदुस्तानी का हाथ तो अंग्रेजी में तंग ही है न । क्या कोई सोचेगा कि क्यों उसे अंग्रेजी के लिए मजबूर किया जाए, क्यों नहीं अंग्रेजीपरस्त ही अपनी हिंदी बेहतर कर लेते हैं, उस बेचारे की खातिर ? खैर, यह सब होने से रहा ।
हिंग्लिश को इंडिया की उदीयमान, तेजी से जड़ें जमाती, और लोकप्रिय होती जा रही क्रिओल भाषा के तौर पर देखा जाना चाहिए । जहां के लोग अब भारत नाम भूलते जा रहे हों और देश को इंडिया बनाने का ख्वाब देख रहे हों, वहां साफ-सुथरी हिंदी के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है । दुर्भाग्य से वहां अंग्रेजी भी नहीं चल सकती है, क्योंकि अधिसंख्य जन उसमें बातचीत नहीं कर सकते हैं । ऐसे में हिंग्लिश क्रिओल ही उपयुक्त विकल्प रह जाता है ।
अस्तु, मैं इस पक्ष का हूं कि हिंग्लिश – एक प्रकार की क्रिओल – को अब मान्यता दे देनी चाहिए । यह अभिजात वर्ग के मुंह पर कब्जा कर चुकी है; अब यह दिन-ब-दिन मजबूत होने जा रही है । आखिर सोचिए उर्दू और हिंदी में अंतर ही कितना है ? जब उर्दू को अलग भाषा का दर्जा मिला हुआ है, तो ठीक उसी तरह – जी हां उसी तरह – हिंग्लिश को मान्यता क्यों न दी जाए ? हिंदी से जितनी दूर उर्दू है उससे कम दूर हिंग्लिश नहीं है ! – योगेन्द्र जोशी
‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ और राजभाषा हिंदीं
अक्टूबर 13, 2009
अगले वर्ष इसी माह (3 से 14 अक्टूबर, 2010) अपने देश, ‘इंडिया’, में ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ (जिन्हें हिंदी में शायद राष्ट्रकुल खेल कहा जाता है) का ‘भव्य’ आयोजन होना है । मेरी शुभकामनाएं आयोजकों के प्रति कि उन्हें इस आयोजन में पूर्ण सफलता मिले तथा वे देश की ‘दांव पर लगी प्रतिष्ठा’ को बचाने में कामयाब रहें । उक्त खेल उत्कंठित देशवासियों तथा उत्सुक खेलप्रेमियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुकूल संपन्न होवें यह मेरी दैवी शक्तियों से प्रार्थना है । (आयोजकों की वेबसाइटः http://www.cwgdelhi2010.org/home.aspx)
 समाचार माध्यमों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि उक्त आयोजन की तैयारियां संतोषजनक नहीं चल रही हैं । खैर तैयारी के बारे में कुछ कह पाना शायद आम नागरिक के लिए संभव नहीं । लेकिन एक बात पर टिप्पणी करने का मेरा भी मन हो आया, जब मेरी नजर संबंधित ‘लोगो’ (क्या कहते हैं इसे, प्रतीकचिह्न ?) पर पड़ी, जिसे यहां इन शब्दों के साथ छाप रहा हूं । मेरी जानकारी में ‘हिंदी’ राजभाषा है, और देवनागरी, न कि रोमन, उसकी लिपि है । मेरे अनुमान से अपने देश की सरकार इस राजभाषा को स्थान देती है, कम से कम मुद्रित सामग्री में । अगर सरकार से पूछा जाय तो यही सुनने को मिलेगा कि राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है और उसे बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं । अगर स्थान नहीं देगी तो राजभाषा किस काम की रह जायेगी भला ? किंतु ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ के लिए जो ‘लोगो’ (logo) प्रयोग में लिया जा रहा है उसमें कहीं एक भी अक्षर देवनागरी का नहीं है, जैसा पहले चित्र से जाहिर है | क्या इस लोगो में अंग्रेजी के साथ देवनागरी में भी वांछित शब्दों का उल्लेख नहीं होना चाहिए था ? लोगो क्या वैसा नहीं हो सकता था जैसा मेरे द्वारा संशोधित दूसरे चित्र में दिखाया गया है ? ऐसा ही कुछ संभव था और है । क्या वजह है कि आयोजकों को राजभाषा से इतना परहेज है ? क्या वजह है कि सरकार राजभाषा के प्रति इतना उदासीन है, लेकिन फिर भी उसे ‘राजभाषा’ खिताब से वंचित करने पर विचार नहीं करती ?
समाचार माध्यमों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि उक्त आयोजन की तैयारियां संतोषजनक नहीं चल रही हैं । खैर तैयारी के बारे में कुछ कह पाना शायद आम नागरिक के लिए संभव नहीं । लेकिन एक बात पर टिप्पणी करने का मेरा भी मन हो आया, जब मेरी नजर संबंधित ‘लोगो’ (क्या कहते हैं इसे, प्रतीकचिह्न ?) पर पड़ी, जिसे यहां इन शब्दों के साथ छाप रहा हूं । मेरी जानकारी में ‘हिंदी’ राजभाषा है, और देवनागरी, न कि रोमन, उसकी लिपि है । मेरे अनुमान से अपने देश की सरकार इस राजभाषा को स्थान देती है, कम से कम मुद्रित सामग्री में । अगर सरकार से पूछा जाय तो यही सुनने को मिलेगा कि राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है और उसे बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं । अगर स्थान नहीं देगी तो राजभाषा किस काम की रह जायेगी भला ? किंतु ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ के लिए जो ‘लोगो’ (logo) प्रयोग में लिया जा रहा है उसमें कहीं एक भी अक्षर देवनागरी का नहीं है, जैसा पहले चित्र से जाहिर है | क्या इस लोगो में अंग्रेजी के साथ देवनागरी में भी वांछित शब्दों का उल्लेख नहीं होना चाहिए था ? लोगो क्या वैसा नहीं हो सकता था जैसा मेरे द्वारा संशोधित दूसरे चित्र में दिखाया गया है ? ऐसा ही कुछ संभव था और है । क्या वजह है कि आयोजकों को राजभाषा से इतना परहेज है ? क्या वजह है कि सरकार राजभाषा के प्रति इतना उदासीन है, लेकिन फिर भी उसे ‘राजभाषा’ खिताब से वंचित करने पर विचार नहीं करती ? 
लोगो में अंकित शब्द वास्तव में प्रथमतः राजभाषा में और तत्पश्चात् उसके साथ अंग्रेजी में होने चाहिए थे, क्योंकि संविधान के अनुसार हिंदी (देवनागरी लिपि में) प्रमुख राजभाषा है और अंग्रेजी उसकी सहायक राजभाषा । सरकारी तंत्र ने घोषित सांविधानिक नीति के विरुद्ध अंग्रेजी को प्रमुख राजभाषा का दर्जा दे रखा है । फिर भी घोषित राजभाषा अंग्रेजी की सहायक राजभाषा के तौर पर तो प्रयुक्त हो ही सकती है । राजभाषा हिंदी के प्रति इतना भी सम्मान अथवा सदाशयता नीतिनिर्धारकों के मन में क्यों नहीं है कि थोड़ा बहुत रस्मअदायगी ही निभा लें ?
एक और बात मेरे जेहन में उठती है । विश्व के अन्य प्रमुख देश खेल और तत्सदृश कोई और आयोजन करते हैं तो पूरी कार्यवाही अंग्रेजी के अतिरिक्त अपनी भाषा में भी प्रस्तुत करते हैं । याद किजिए जब चीन में ओलंपिक खेल संपन्न हुए थे । अपने देश में क्या होगा ? क्या उक्त खेलों के अवसर पर कहीं देवनागरी लिखी देखने को मिलेगी ? कहीं हिंदी लफ़्ज़ सुनने को मिलेंगे ? मुझे शंका है कि उस मौके पर भी अपनी राजभाषा सदा की तरह तिरस्कृत ही रहेगी ।
मुझे अंग्रेजी के प्रयोग पर आपत्ति नहीं है । विश्व में अन्य देश भी इसको महत्त्व दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी मौलिक भाषाओं को ही भूल जाएं । प्रमुख देशों में कोई ऐसा नहीं होगा जहां अपने देश की भाषा को शासित प्रजा की भाषा के तौर पर देखा जाता हो और अंग्रेजी को शासकों की भाषा बने रहने दिया जा रहा हो । देश में दो प्रकार की भाषाएं हैं, एक आम जन की देसी भाषाएं और दूसरे अंग्रेजी जो आज भी देश पर राज करने वालों की भाषा है, ठीक वैसे ही जैसे विदेशी राज में था । राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होने के बावजूद इस देश का शासक वर्ग स्वयं को आम जनता से ऊपर मानता है और अपने को उनसे अलग रखने के लिए अंग्रेजी का हथियार इस्तेमाल करता आ रहा है । क्या ऐसी मानसिकता वाले शासकों से यह देश कभी मुक्त हो सकेगा ? शायद कभी नहीं ! – योगेन्द्र जोशी
दक्षिण भारत यात्रा और हिंदीः चतुर्थ भाग, केरल और हिंदी
अप्रैल 14, 2009
मेरी अभी तक की दक्षिण भारत यात्राएं मुख्यतया तमिलनाडु के नगरों/पर्यटक स्थलों से संबंधित रही हैं । मैं त्रिवेंद्रम, मैसूर, बेंगलुरु, और तिरुपति भी हो आया हूं, किंतु केवल एक या दो बार । लेकिन चेन्नै जाना प्रायः हर बार हुआ है । सन् १९७३ की पहली से अभी हाल में संपन्न यात्रा तक हिंदी को लेकर मैंने वहां क्या अनुभव किया और क्या परिवर्तन देखे इसकी चर्चा मैंने पिछले चिट्ठों में की है । पहली यात्रा के समय एक केरलवासी के साथ चेन्नै (तब मद्रास) में हुयी बातचीत का जिक्र भी ९ फरवरी (२००९) की पिछ्ली पोस्ट में शामिल है ।
कोई चार-एक साल पहले वाराणसी से रेलयान द्वारा तिरुपति जाते समय भी मुझे केरल के दो जनों से वार्तालाप का अवसर मिला था । वे दोनों कोचीन विश्वविद्यालय (जैसा मुझे याद है) में बतौर अध्यापक कार्यरत थे और हिंदी विषय पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आयोजित एक सम्मेलन में भाग लेकर लौट रहे थे । रेलगाड़ी में बैठे-बैठे बिताये उस दो-दिनी यात्रा में मेरी उनके साथ विभिन्न विषयों पर अच्छी-खासी बातचीत हुई थी जिसका पूरा विवरण मस्तिष्क-पटल पर अब नहीं रह गया है । फिर भी वार्तालाप के कुछ अंश याद हैं ।
उन विद्वज्जनों ने मुझे बताया कि केरल में हिंदी काफी लोकप्रिय है । उनका कहना था कि वहां माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र के अनुसार पढ़ाई चल रही है, अतः हिंदी का कामचलाऊ ज्ञान अधिकांश छात्रों को हो जाता है । उन्होंने बताया कि उनके विश्वविद्यालय में एम.ए. के पाठ्यक्रम में केवल २० सीटें उपलब्ध हैं, किंतु उसमें प्रवेश के लिए प्रायः २०० प्रार्थनापत्र आ जाते हैं । पाठ्यक्रम की मांग अच्छी है और उनका विश्वविद्यालय अधिकांश छात्रों की मांग पूरी नहीं कर सकता है । वहां कुछ कालेजों में बी.ए. (हिंदी स्नातक) तक पढ़ाई संभव है, लेकिन स्नातकोत्तर की पढ़ाई केवल कुछ ही संस्थाओं में हो सकती है । उनके अनुसार कुछ छात्रों का हिंदी के प्रति रुचि का कारण नौकरी-पेशे में लाभ की संभावना रहा है । आजकल अनुवादकों की मांग भी देखने को मिल रही है । मलयालम और अंगरेजी के साथ हिंदी की जानकारी उपयोगी सिद्ध होती है ।
मेरा यह अनुमान है कि हिंदी सीखना तमिलभाषियों की तुलना में मलयालमभाषियों के लिए अपेक्षया अधिक सरल है । इसका कारण मेरी दृष्टि में यह है कि मलयालम में संस्कृत मूल के शब्दों की संख्या काफी है, कदाचित् हिंदी से भी अधिक । मेरी जानकारी के अनुसार दक्षिण की तीन भाषाओं, कन्नड़ (Kannad), तेलुगू (Telugu) तथा मलयालम (Malayalam), में संस्कृत मूल के शब्दों की संख्या अच्छी-खासी है । रोजमर्रा की सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त इन भाषाओं के शब्द अवश्य ही सर्वथा भिन्न हैं, किंतु किसी विषय की गंभीर तथा विद्वत्तापूर्ण चर्चा या समीक्षा के लिए आवश्यक उन्नत दर्जे की अभिव्यक्ति में प्रयुक्त शब्द-संपदा काफी हद तक संस्कृत पर आधारित है । भाषाविद् इन तीनों तथा तमिल (Tamil) को सम्मिलित तौर पर द्रविड़ (Dravidian) भाषा कहते है और उनकी राय में ये संस्कृत से कमोबेश असंबद्ध हैं । उनके मत में संस्कृत का यूरोपीय भाषाओं (Indo-European) से कहीं अधिक निकटता का संबंध है । अवश्य ही उनका मत सुविचारित एवं गंभीर तर्कों पर आधारित होगा, किंतु मैं उनके मत हो स्वीकारने में हिचकिचाता हूं । मैंने जब इन दक्षिण भारतीय भाषाओं की लिपियों पर नजर दौड़ायी और देवनागरी से उनकी तुलना की तो मुझे आशा से कहीं अधिक समानता देखने को मिली । इस तुलना को मैंने ‘वर्णमाला’ (Alphabet, यहां क्लिक करें) नाम के ‘पेज’ में प्रस्तुत किया है । यद्यपि मैं इन भाषाओं के व्याकरण से अभी परिचित नहीं हो सका हूं, तथापि मुझे उम्मींद है कि उस दृष्टि से भी कुछ हद तक साम्य होगा, कदाचित् यूरोपीय भाषाओं से अधिक । कहने का तात्पर्य यह है कि लिप्यात्मक समानता भाषाएं सीखने में मदद करती है, और इसलिए कन्नड़, तेलुगू तथा मलयालम जानने वालों के लिए हिंदी सीखना अधिक कठिन नहीं होना चाहिए ।
 रॉक मेमॉरिअल से कन्याकुमारी का पैनॉरॅमिक दृश्य
रॉक मेमॉरिअल से कन्याकुमारी का पैनॉरॅमिक दृश्य
अस्तु, मेरा अनुमान है कि केरलवासी हिंदी में अपेक्षया अधिक रुचि रखते हैं, कारण भले ही कुछ भी हों । कन्याकुमारी की पिछली यात्रा के समय मैं आसपास के पर्यटक स्थलों को भी देखने गया था, जिनमें ‘रामनाथपुरम्’ का रामलिंगविलास राजमहल भी एक था । यह भवन कभी ट्रावनकोर के राजा का महल हुआ करता था और अब एक धरोहर-संग्रहालय है । इसे काष्ठ महल (Wooden Palace) के नाम से भी जाना जाता है । यह स्थान है तो तमिलनाडु राज्य में, परंतु महल तथा उसके परिसर पर केरल सरकार का प्रशासनिक नियंत्रण है । संग्रहालय के विभिन्न पहलुओं तथा वहां संगृहीत वस्तुओं के बारे में संक्षिप्त जानकारी आपको प्रायः मलयालम, हिंदी तथा अंग्रेजी, तीनों, भाषाओं में मिल जायेगी । मैंने पिछली पोस्ट में कहा था कि चेन्नै में अबस्थित केंद्र सरकार के संग्रहालय में लिखित हिंदी बमुश्किल देखने को मिलती है । केरल तथा तमिलनाडु में हिंदी के प्रति व्याप्त रवैये में अंतर देखने को मिलता है ।
 रामलिंगविलास राजमहल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु
रामलिंगविलास राजमहल, रामनाथपुरम, तमिलनाडु
संदर्भगत क्षेत्र की यात्रा के समय मिले हिंदी से जुड़े हुए अनुभवों की शेष बातें अगली (अंतिम) पोस्ट में प्रस्तुत की जायेंगी । – योगेन्द्र
 ‘वुडन रूफ़ कार्विङ्’, रामलिंगविलास, रामनाथपुरम्
‘वुडन रूफ़ कार्विङ्’, रामलिंगविलास, रामनाथपुरम्
दक्षिण भारत यात्रा और हिंदीः तृतीय भाग, बदलाव के संकेत
मार्च 31, 2009
पिछली पोस्ट (मार्च १, २००९) के आगे । मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि मेरी पहली दक्षिण-भारत यात्रा (१९७३) के दौरान हिंदी को लेकर हुआ अनुभव निराशाप्रद रहा उसके बाद मैं दूसरी बार १९८० में भी वहां गया था । तब स्थिति कुछ अनुकूल लगी थी । उसके बाद के लंबे अंतराल में पांच-छः बार उस क्षेत्र में जा चुका हूं । चार-पांच साल पहले की और फिर विगत फरवरी की यात्राएं कुछ हद तक आशाप्रद रहीं मैं ऐसा कह सकता हूं ।

एक बात मैं आंरभ में ही स्पष्ट कर दूं कि हिंदी देश की राजभाषा घोषित होने के बावजूद दस्तावेजी भाषा नहीं बन सकी है । अवश्य ही इसका देश के कोने-कोने तक कुछ हद तक फैलाव हो रहा है, और यह भी कहा जा सकता है कि अधिकाधिक लोग इसे समझने लगे हैं और थोड़ा-बहुत, टूटी-फूटी ही सही, इसे बोलने भी लगे हैं । लेकिन लिखित रूप में इसे कम ही लोग इस्तेमाल में ले रहे हैं । और तो और खुद हिंदीभाषी भी लिखित हिंदी में नाममात्र की रुचि रखते हैं । इस माने में उनकी प्राथमिकता अंग्रेजी ही रहती आ रही है । अतः जब में हिंदी की किंचित् आशाप्रद स्थिति की बात करता हूं तो इसका मतलब मात्र यह है कि अब नये क्षेत्रों में भी बोलने-चालने के स्तर पर इसकी मौजूदगी देखी जा सकती है । दक्षिण भारत के कुछ शहरी इलाकों में हिंदी बोलकर आप कुछ हद तक काम चला सकते हैं । लेकिन लिखित तौर पर इसे आप शायद ही कहीं देखें । आपको हिंदी पत्र-पत्रिकाएं खोजने पर बमुश्किल ही मिलेंगे । केंद्र सरकार के उपक्रमों के नामपट्टों को छोड़ इक्के-दुक्के स्थलों पर लिखित हिंदी दिखेगी । आगे पढ़ने के लिए यहां >> क्लिक करें
दक्षिण भारत यात्रा और हिन्दी: द्वितीय भाग, चेन्नै में
मार्च 1, 2009
 कन्याकुमारी – विवेकानंद रॉक मेमॉरिअल, शिला स्मारक
कन्याकुमारी – विवेकानंद रॉक मेमॉरिअल, शिला स्मारक
जब मैं पहली बार (जुलाई १९७३ में, जैसा मुझे याद है) चेन्नै, यानी तत्कालीन मद्रास, गया था तो मुझे वहां हिन्दी के विरुद्ध एक प्रकार का द्वेष या उदासीनता का भाव देखने को मिला था । रेलवे स्टेशन पर हिन्दी में जानकारी पाना मुझे असंभव-सा लगा था । पूछताछ कार्यालय और टिकट खिड़की पर हिन्दी में कुछ पूछने पर संबंधित कर्मचारी के मुख पर एक प्रकार की नाखुशी का भाव मुझे देखने को मिला था । उस समय मैं स्वयं हिन्दी के प्रति विशेष जागरूक नहीं था और अंग्रेजी के प्रयोग से बचने का विचार भी मेरे मन में नहीं हुआ करता था । (हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रति मौजूदा विचार कई वर्षों बाद मेरे मन में उपजे थे ।) सच तो यह है कि हिन्दी के प्रति वहां व्याप्त विरोध-भाव तब मेरे लिए चिंता या चिंतन का विषय ही नहीं था । अंग्रेजी से मेरा काम उस समय चल गया था और मैं संतुष्ट था । यह तो आज है कि मैं उस घटना को नये नजरिये से देखता हूं ।
वह ऐसा समय था जब तमिलनाडु में कुछ काल पहले लगी हिन्दी-विरोध की आग शांत नहीं हुयी थी । वस्तुतः उस राज्य में हिन्दी विरोध काफी पुराना रहा है । विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह विरोध १९३८ से ही वहां चलता आ रहा था । ध्यान दें कि वर्ष १९५० में संविधान संशोधन के द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था । शेष के लिए यहां >> क्लिक करें
विवादित परिभाषाएं, दो: धर्मनिरपेक्षता,…
दिसम्बर 22, 2008
विगत पोस्ट (११ दिसंबर, २००८) के आगे ।
धर्मनिरपेक्षता – राजनीति के क्षेत्र में यह शब्द बहुधा सुनने को मिलता है और उसी के परिप्रेक्ष में बुद्धिजीवी वर्ग भी इस पर चर्चाएं करता आया है । मैं समझता हूं कि अपने देश में इस शब्द की महत्ता हाल के वर्षों में बहुत बढ़ गयी है, और राजनेताओं के लिए यह जनसामान्य को भ्रमित करके अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करने का एक अच्छा हथियार बन चुका है । मेरी समझ में हर कोई इस शब्द की व्याख्या सुविधानुसार और मनमाने तरीके से कर रहा है ।
क्या है धर्मनिरपेक्षता ? अपने देश में यह अंग्रेजी के ‘सेक्युलर’ (secular) के लिए हिन्दी का समानार्थी शब्द के तौर पर प्रयोग में लिया जा रहा है । शब्दकोष सेक्युलर के अर्थ यूं देते हैं: “1. denoting attitudes, activities, or other things that have no religious or spiritual basis; 2. not subject to or bound by religious rules; not belonging to or living in a monastic or other order.” (अभिवृत्तियां/रवैया, कर्म/कार्य, अथवा अन्य बातें जिनका आधार धार्मिक या आध्यात्मिक न हो; धार्मिक नियमों के अधीन या उनसे बंधा हुआ न हो; मठ-आवासीय या अन्य प्रकार के नियमों से असंबद्ध, अथवा तदनुरूप जीवनयापन से परे; संदर्भ: Oxford Dictionary of Difficult Words)”
हिन्दीः निजी अनुभव – 2
सितम्बर 26, 2008
पिछली शताब्दि के अंतिम दशक के आरंभ के आसपास अपने यूरोपीय अनुभव से प्रेरित होकर मैंने निर्णय लिया कि मैं जहां-जहां संभव हो सके वहां-वहां हिन्दी का प्रयोग करूं । किसी परिचित, मित्र, सहकर्मी अथवा अधिकारी से किसी भी प्रकार का प्रोत्साहन अथवा उत्साहवर्धन मुझे मिला हो ऐसा नहीं है । बल्कि मैं समझता हूं कि कई लोगों को मेरी बातें सनक भरी ही लगती रही होंगी । हां, खुलकर किसी ने नकारात्मक टिप्पणी की हो ऐसा नहीं है ।
मेरे कार्यक्षेत्र रहे विश्वविद्यालय में प्रायः सभी दस्तावेजी या लिखित कार्य अंग्रजी में ही होते हैं और उन दिनों भी होते थे, भले ही वहां कार्यरत निचले स्तर के कुछेक कर्मचारियों के लिए वह सब समझ से परे हो । मुझे एक वाकया याद है जब मेरे विभागीय कार्यालय का एक चपरासी एक बार एक नोटिस मेरे पास ले आया, जिसके साथ अध्यापकों की सूची की जीराक्स प्रति (अक्सर इस्तेमाल होने वाली) भी थी । सूची में उन-उन अध्यापकों के नामों के आगे निशान लगे थे जिनको वह नोटिस दिखायी जानी थी । मेरे नाम के आगे निशान नहीं लगा था । मैंने उस व्यक्ति को बताया कि बिल्डिंग के एक कोने में स्थित मेरे कमरे तक आने की जहमत उठाने की उसे जरूरत नहीं थी और यह भी कि जिन के नाम पर टिक किया था केवल उन्हीं के पास उसे जाना चाहिए । उसने मुझे बताया कि वह अंग्रेजी में लिखे नाम तो पढ़ नहीं सकता और उतने सारे लोगों का नाम याद रख पाना उसके लिए कठिन था । कहीं किसी नाम छूट जाये तो ख्वाहमख्वाह ही उसे डांट सुननी पड़ेगी ।
अवश्य ही अंग्रेजी का अतिशय प्रयोग, वह भी उन स्थलों पर जहां हिन्दी अधिक सुविधाजनक हो, मुझे स्वीकार्य नहीं था । मैंने सोचा कि अध्यापकों की सूची क्यों न हिन्दी में तैयार कर ली जाये । मैंने यह कार्य अपने ही जिम्मे ले लिया क्योंकि मुझे मालूम था कि यदि कार्यालय वालों पर छोड़ दिया तो कुछ भी होने से रहा । अतः दो-चार दिन के भीतर मैंने कंप्यूटर पर सूची तैयार की और बड़े बाबू को सोंप दी, ताकि वे उसकी जीराक्स कापी प्रयोग में ले सकें ।
कुछ वर्षों तक तो सब ठीक-ठाक चलता रहा । सालों तक कोई नियुक्ति भी नहीं हुयी, अतः सूची अपरिवर्तित रही । फिर शताब्दि का अंत आते-आते कुछ नये लोग विभाग में नियुक्त हुए । आरंभ में तो उनके नाम हाथ से अंग्रेजी में लिखे जाने लगे और अंत में नयी सूची अंग्रेजी में तैयार हो गयी । मेरा भी उस दिशा में उत्साह ठंडा पड़ गया क्योंकि मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का मन बना लिया था ।
लेकिन मेरा कार्य वैयक्तिक स्तर पर यथासंभव हिन्दी में चलता रहा । जैसा मैंने बताया कि वहां सब कुछ तो अंग्रेजी में था । राजभाषा के नियमों के अनुसार सभी फार्म द्विभाषी होने चाहिए । लेकिन ऐसा आज तक नहीं हुआ है । मैंने अपने समय में कई बार विश्वविद्यालय को याद दिलाया कि हिन्दी में भी फार्म उपलब्ध होने चाहिए । हर बार किसी न किसी बहाने प्रशासन टालता रहा । परंतु मैंने निर्णय लिया कि अंग्रेजी में छपे फार्मों की प्रविष्टयां मैं हिन्दी में ही भरूंगा । ऐसा मैं करता रहा । मेरा पत्राचार भी हिन्दी में होने लगा । मैंने जब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का आवेदन पेश किया तो वह भी हिन्दी में ही लिखा । लेकिन उन सभी पत्रों आदि पर संबद्ध अधिकारियों की टिप्पणियां अंग्रेजी में ही हुआ करती थीं, जो कि राजभाषा नियमों के विरुद्ध था । पर परवाह किसे थी ?
मैंने तब अनुभव किया कि दो-चार लोग हों तो शायद कुछ किया जा सकता था । पर जिस तंत्र में सभी अंग्रेजी के प्रति समर्पित हों और उसके परे कुछ भी करने का विचार न रखते हों, वहां भला क्या हो सकता है ? भाषा के मामले में लोग क्यों जड़त्व से ग्रस्त हैं इस पर आगे चर्चा की जायेगी । – योगेन्द्र