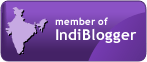राजभाषा हिन्दी चर्चा में है, कारण मोदी सरकार द्वारा विभागों को दिए गए निर्देश कि वे राजकीय कार्य प्रमुखतया हिन्दी में करें । हिन्दी भारतीय संघ की संविधान-सम्मत राजभाषा है, यानी राजकाज की भाषा । लेकिन संविधान की बात-बात पर दुहाई देने वाले हमारे अधिकांश राजनेता चाहते हैं कि राजकाज मुख्यतः अंगरेजी में ही होते रहना चाहिए और वह भी भविष्य में सदैव के लिए । मैं समझ नहीं पाता कि जब हिन्दी का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए, या मात्र खानापूर्ति भर के लिए हो, तब हिन्दी को राजभाषा बनाए रखने का तुक ही क्या है ? लेकिन इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत भी ये नेता महसूस नहीं करते ।
हिन्दी का विरोध उस समय भी हुआ था जब इसे राजभाषा के खिताब से नवाजा जा रहा था । उस काल में अंततोगत्वा संविधान-निर्माण में लगे नेतावृंद सहमत हो ही गये, हिन्दी के साथ सीमित समय के लिए अंगरेजी भी बनाए रखने की शर्त के साथ । वह सीमित समय विगत 63-64 सालों के बाद भी घटने के बजाय अनंतकाल की ओर बढ़ता जा रहा है । पिछली शताब्दी के पचास-साठ के दशकों में विरोध के सर्वाधिक जोरशोर के स्वर तमिल राजनेताओं ने उठाए थे । और आज भी उनका वह विरोध लगभग जैसा का तैसा बरकरार है । उन्होंने शायद कसम खा रखी है कि हिन्दी को लेकर हम न अभी तक बदले हैं और न ही आगे बदलेंगे ।
हिन्दी का जैसा विरोध पचास-साठ के दशक में था वैसा कदाचित अब नहीं रहा । हिन्दी के प्रति तमिलभाषियों का रवैया काफी-कुछ बदल रहा है, भले ही राजनैतिक कारणों से नेताओं का रवैया खास न बदला हो । यों भी इतना जबरदस्त विरोध किसी और राज्य में न तब था और न अब है । वस्तुतः यह तथाकथित तमिल स्वाभिमान से जुड़ा है, ऐसा स्वाभिमान जो अन्यत्र देखने को नहीं मिलता । सवाल उठता है कि इस स्वाभिमान को अंगरेजी से कोई खतरा क्यों नहीं होता । मैंने अनुभव किया है कि तमिलनाडु के ही पड़ोसी राज्य केरल में स्थिति आरंभ से ही बहुत कुछ भिन्न रही है, पचास-साठ के दशक में और आज भी ।
इस संबंध में मुझे 1973 की दक्षिण भारत की यात्रा का अनुभव याद आता है । जून-जुलाई का समय था । तब अध्यापन एवं अनुसंधान के क्षेत्र में मेरा नया-नया व्यावसायिक प्रवेश हुआ था । मुझे उच्चाध्ययन से संबंधित कार्य हेतु बेंगलूरु-स्थित आईआईएससी संस्थान में एक माह के लिए ठहरना था । उस काल में बेंगलूरु बंगलोर कहलाता था ।
रेलगाड़ी से बेंगलूरु पहुंचने के लिए मैं पहले चेन्नै (तब मद्रास) पहुंचा रात्रि प्रथम प्रहर । मुझे अगले दिन प्रातःकालीन गाड़ी से बेंगलूरु जाना था । वयस्क जीवन के उस आंरभिक काल तक मुझे लंबी यात्राओं, विशेषतः दक्षिण भारत की यात्राओं, का कोई अनुभव नहीं था । तब रेलगाड़ियों में आरक्षण कराना भी आसान नहीं होता था । दूसरे शहरों से आरंभ होने वाली यात्राओं का आरक्षण आप आज की तरह आसानी से नहीं करा सकते थे । तब रेलवे विभाग इस कार्य को तार (टेलीग्राम) द्वारा संपन्न किया करता था, जिसके परिणाम बहुधा नकारात्मक मिलते थे । हां, आजकल की जैसी भीड़भाड़ तब रेलगाड़ियों में कम ही होती थी ।
मैंने वह रात वहीं प्रतीक्षालय में बिताई, एक किनारे जमीन पर चादर बिछाकर । रेलगाड़ियों के इंतिजार में प्रतीक्षालयों और प्लेटफॉर्मों पर लेटे अथवा सोते हुए समय गुजारना भारतीय यात्रिकों के लिए आज भी आम बात है । तभी वहां मेरे ही नजदीक एक प्रौढ़ सज्जन आकर आराम फरमाने लगे । कुछ काल की चुप्पी के पश्चात नितांत अजनबी होने के बावजूद हम एक दूसरे की ओर मुखातिब हुए और कौन कहां से आया है और कहां जा रहा है जैसे सवालों के माध्यम से परस्पर परिचित होने लगे । यह भारतीय समाज की विशिष्टता है कि रेल-यात्राओं के दौरान जब दो अपरिचित जन आसपास बैठे हों तो वे अधिक देर तक चुपचाप नहीं रहते और किसी भी बहाने परस्पर वार्तालाप पर उतर आते हैं । अपने देश के अभिजात वर्ग में पाश्चात्य समाजों की भांति ऐसा कम ही देखने को मिलता है । हमारे शहरी जीवन में लोग अब इस मामले में अभिजात बनते जा रहे हैं । अस्तु ।
उन सज्जन से मेरी बातचीत का सिलसिला अंगरेजी में आंरभ हुआ । जब मैंने अपने शहर और गंतव्य के बारे में बताया तो वे अंगरेजी से हिंदी पर उतर आये । इधर हिन्दी तो चलती नहीं होगी अपनी इस धारणा को उनके समक्ष रखते हुए मैंने उनकी हिन्दी पर आश्चर्य व्यक्त किया । लगे हाथ उनकी यात्रा संबंधी अन्य बातें भी उनसे जाननी चाहीं ।
उन्होंने मुझे बताया कि वे केरला के रहने वाले हैं और अपने कारोबार के सिलसिले में गुवाहाटी के लिए निकले हैं । बातचीत से पता चला कि उन्हें कारोबार के सिलसिले में आसाम तक के कई राज्यों में जाना होता है । उनका कहना था कि इन सभी जगहों पर कारोबारी बातें अंगरेजी के बदले हिन्दी में करना आसान होता है । सभी प्रकार के लोग मिलते हैं, कई ऐसे भी जो अंगरेजी में ठीक से बात नहीं कर सकते ।
उस समय मैंने उनसे उनके कारोबार के बारे में पूछा या नहीं इसका ध्यान नहीं । मेरे लिए यह समझना अधिक अहम था कि सुदूर दक्षिण के दो पड़ोसी राज्यों, तमिलनाडु और केरला, में हिन्दी के प्रति एक जैसा रवैया नहीं है । मैं चेन्नै स्टेशन पर यह देख चुका था कि हिन्दी में बात करने पर अधिकांश रेलवे कर्मचारियों के चेहरों पर तिरस्कार के भाव उभर आते हैं । मैंने उनको बताया कि मैं मद्रास पहली बार आया हूं । यहां के हिन्दी-विरोध की बातें मैंने सुन रखी थीं, और इस यात्रा में उसका थोड़ा अनुभव भी हुआ है । मैंने उनके सामने आशंका जताई कि ऐसा विरोध केरला में भी होता होगा ।
उनका उत्तर नहीं में था । उनका कहना था कि केरला के लोग व्यावहारिक सोच रखते हैं । रोजी-रोटी के लिए वे लोग देश के अलग-अलग हिस्सों तक पहुंचते हैं और देश के बाहर भी जाते हैं । वे जानते हंै कि हिन्दी से परहेज करके उन्हें कोई लाभ नहीं होने का ।
मेरा दक्षिण भारत जाना कई बार हो चुका है । हिन्दी को लेकर हर बार मुझे पहले से बेहतर अनुभव हुए हैं । चेन्नई में आज भी हिन्दी अधिक नहीं चलती है, लेकिन उसी राज्य के रामेश्वरम एवं कन्याकुमारी में आपको कोई परेशानी नहीं होती । केरला में हिन्दी के प्रति लोगों का झुकाव है यह बात मुझे एक बार वहां के दो शिक्षकों ने बताई थी जिसका उल्लेख मैंने अपनी अन्य पोस्ट में किया है । इसका मतलब यह नहीं कि वहां हर कोई हिन्दी जानता हो । किसी भाषा का अभ्यास एवं प्रयेाग के पर्याप्त अवसर होने चाहिए जो आम आदमी को नहीं होते । लेकिन विरोध जैसी कोई चीज वहां सामान्यतः नहीं है । – योगेन्द्र जोशी
दक्षिण भारत यात्रा और हिन्दी: द्वितीय भाग, चेन्नै में
मार्च 1, 2009
 कन्याकुमारी – विवेकानंद रॉक मेमॉरिअल, शिला स्मारक
कन्याकुमारी – विवेकानंद रॉक मेमॉरिअल, शिला स्मारक
जब मैं पहली बार (जुलाई १९७३ में, जैसा मुझे याद है) चेन्नै, यानी तत्कालीन मद्रास, गया था तो मुझे वहां हिन्दी के विरुद्ध एक प्रकार का द्वेष या उदासीनता का भाव देखने को मिला था । रेलवे स्टेशन पर हिन्दी में जानकारी पाना मुझे असंभव-सा लगा था । पूछताछ कार्यालय और टिकट खिड़की पर हिन्दी में कुछ पूछने पर संबंधित कर्मचारी के मुख पर एक प्रकार की नाखुशी का भाव मुझे देखने को मिला था । उस समय मैं स्वयं हिन्दी के प्रति विशेष जागरूक नहीं था और अंग्रेजी के प्रयोग से बचने का विचार भी मेरे मन में नहीं हुआ करता था । (हिन्दी और भारतीय भाषाओं के प्रति मौजूदा विचार कई वर्षों बाद मेरे मन में उपजे थे ।) सच तो यह है कि हिन्दी के प्रति वहां व्याप्त विरोध-भाव तब मेरे लिए चिंता या चिंतन का विषय ही नहीं था । अंग्रेजी से मेरा काम उस समय चल गया था और मैं संतुष्ट था । यह तो आज है कि मैं उस घटना को नये नजरिये से देखता हूं ।
वह ऐसा समय था जब तमिलनाडु में कुछ काल पहले लगी हिन्दी-विरोध की आग शांत नहीं हुयी थी । वस्तुतः उस राज्य में हिन्दी विरोध काफी पुराना रहा है । विकीपीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह विरोध १९३८ से ही वहां चलता आ रहा था । ध्यान दें कि वर्ष १९५० में संविधान संशोधन के द्वारा हिन्दी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था । शेष के लिए यहां >> क्लिक करें
दक्षिण भारत यात्रा और हिन्दी: प्रथम भाग
फ़रवरी 19, 2009
सुदूर दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के दो-एक पर्यटक स्थलों की दश-द्वादश-दिवसीय यात्रा के पश्चात् मैं अभी हाल ही में लौटा हूं । मैं पारिवारिक सदस्यों के चार जनों के दल में शामिल था । हम लोग चेन्नै होते हुए रामेश्वरम्, कन्याकुमारी तथा मदुरै तक हो आये और फिर चेन्नै दो दिन रुककर वापस वाराणसी लौट आये । इस आलेख में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत करना मेरा इरादा नहीं है; मैं हिन्दी को लेकर अर्जित अपने अनुभवों का उल्लेख भर करना चाहता हूं ।
मेरे लिए तमिलनाडु के उक्त स्थलों की यात्रा कोई नयी बात नहीं थी । मैंने आज से करीब पैंतीस वर्ष पूर्व, यानी उन्नीस सौ तिरहत्तर, में पहली बार इन नगरों का दर्शन किया था । तब से अब तक मैं कुल पांच बार कन्याकुमारी और तीन-तीन बार रामेश्वरम् एवं मदुरै की यात्रा कर चुका हूं । हर बार आना-जाना चेन्नै के रास्ते ही हुआ है, जहां मैं अन्य मौकों पर भी गया हूं । पैंतीस सालों के लंबे अंतराल में कन्याकुमारी नगरी उल्लेखनीय रूप से बदल चुकी है । थोड़ा बहुत बदलाव तो रामेश्वरम् में भी स्वाभाविक रूप से हुआ ही है । हिन्दी संबंधी मेरा अब तक वहां क्या अनुभव रहा इस बात की चर्चा मैं एक अजनबी से अपनी मुलाकात के जिक्र के साथ करता हूं, जो चेन्नै (तत्कालीन मद्रास) सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर तब हुई थी जब मैं पहली बार वहां गया था । पूरा वाकया कुछ यूं है:- (आगे पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें)