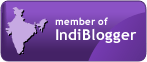अब आप इंटरनेट वेब साइटों (अंतरजाल स्थलों?) के पतों को लैटिन/रोमन लिपि के बदले विश्व की तमाम अन्य मान्य लिपियों में चुन सकते हैं । इस आशय का एक समाचार (क्लिक करें) मुझे इंग्लैंड से छपने वाली पत्रिका ‘न्यू साइंटिस्ट’ (http://www.newscientist.com/) से मिला है ।

यहां पर मैं पत्रिका में छपे पूरे पाठ्य का उल्लेख नहीं कर रहा हूं, केवल कुछ बिंदुओं का सार लिख रहा हूं । उसके पश्चात् अपनी कुछएक टिप्पणियां । पत्रिका का आरंभिक अनुच्छेद इन शब्दों से आरंभ होता है:
आज इंटरनेट का भविष्य कुछ अधिक ही स्पष्ट हो गया है, जब इसकी नियामक संस्था, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – http://www.icann.org/en/general/background.htm), ने लैटिन से भिन्न लिपि-चिह्नों में वेब पतों को लिखने को मान्यता प्रदान कर दी । संस्था के अध्यक्ष, पीटर डेन्गेट थ्रश (Peter Dengate Thrush), समझाते हैं, “अभी तक इंटरनेट पतों का अंतिम अंश लैटिन कैरेक्टरों, A to Z, तक सीमित था ।” उनका आशय था कि अभी तक चीनी वेब नामों का आंरभिक अंश भले ही चीनी कैरेक्टरों में लिखा जा सकता था, उनका अंतिम अंश अनिवार्यतः ‘.cn‘ आदि ही हो सकता था । लेकिन अब …
लेख में लिखा है कि 16 नवंबर से सभी देश अब अपना ‘कैरेक्टर’ समुच्चय पंजीकृत कराकर ‘इंटर्नैशनल डोमेन नेम’ (IDNs) चुन सकेंगे । आगे यह भी कि चीनी भाषा-लिपि की वेब साइट Sun0769 में प्रस्तुत पाठ्य का ‘गूगल’ अनुवाद दावा करता है कि अब ‘लैटिन’ का एकछत्र सामाज्य समाप्त हुआ । जो लोग अंग्रेजी तो दूर उसकी लिपि तक से अपरिचित हैं उनके लिए यह खबर राहत पहुंचाने वाली है यह कहना है चीन की सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी HiChina के वरिष्ठ परियोजना प्रबंधक वांग पेंग (Wang Peng) का । वेब पते का आरंभिक अंश http:// यथावत् बना रहेगा, यद्यपि आजकल इसका लिखा होना आवश्यक नहीं । इंटरनेट की मूल कार्यप्रणाली इस सब से बदलेगी नहीं, कुछ तकनीकी फेरबदल शायद कहीं करना पड़े ।
उक्त लेख में इस रोचक एवं अहम बात का जिक्र है कि आज के समय में चीन में इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है – 33 करोड़ (अमेरिका की जनसंख्या, करीब 31 करोड़, से अधिक !)
वेब नामों में लैटिन लिपि की अनिवार्यता की समाप्ति की जानकारी मुझे गूगल के एक समूह (गूगल ग्रूप) के रास्ते श्री लोचन मखीजा महोदय से भी 4-5 दिन पहले मिली थी ।
चीन की भूमिका
लिपि संबंधी अनिवार्यता समाप्त करने की मांग चल रही है और देर-सबेर लैटिन का वर्चस्व समाप्त हो जायेगा इसका अंदाजा मुझे काफी पहले से था । वस्तुतः करीब तीन साल पहले मेरी नजर में एक लेख (http://www.icann.org/en/announcements/idn-tld-cdnc.pdf) आया था, जिसमें चीन के तत्संबंधी प्रयासों का जिक्र था ।
इसमें दो राय नहीं है कि लैटिन की अनिवार्यता समाप्त करने में चीन की भूमिका सर्वोपरि रही है । जैसा पहले कहा गया है चीन में इंटरनेट उपयोक्ताओं की संख्या सर्वाधिक ही नहीं है बल्कि एक प्रकार से आश्चर्यजनक भी है – 33 करोड़, पूरी जनसंख्या का लगभग 25 प्रतिशत । चीन में अंग्रेजी नहीं चलती है, कम से कम उस तरीके से और उस सीमा तक नहीं जैसे अपने देश तथा पूर्व में ब्रिटिश उपनिवेश रह चुके कई अन्य देशों में । यह बात अधिकांश हिंदुस्तानियों के गले नहीं उतर पाएगी कि वहां अंग्रेजी वास्तव में नहीं चलती । अंग्रेजी जानने वाले चीनियों की संख्या बहुत कम है; इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार करोड़ भर भी नहीं । जो जानते भी हैं उनकी अंग्रेजी कामचलाऊ ही कही जायेगी, अच्छी एवं प्रभावित करने वाली तो शायद ही देखने को मिले । 33 करोड़ की जनता तो अंग्रेजी अल्फाबेट से भी ठीक से परिचित नहीं । फिर इंटरनेट का उपयोग वे भला कैसे कर सकते हैं ? साफ जाहिर है कि वहां के लोग अंग्रेजी नहीं, बल्कि अपनी चीनी – असल में मैंडरिन – के माध्यम से ही इंटरनेट का प्रयोग कर रहे हैं । चीन ने इस बात को महत्त्व दिया कि उसके अधिकाधिक लोग इंटरनेट का भरपूर प्रयोग करें और इस कार्य में अंग्रेजी उनके लिए रोड़ा न बने । यहां तक कि वेब साइटों के नाम लैटिन में लिखने की बाध्यता से भी उसकी जनता मुक्त रहे यह चीन का लक्ष्य रहा है । कुछ भी हो यह मानता पड़ेगा कि आईसीएएनएन के प्रसंगगत निर्णय के पीछे चीन की भूमिका प्रमुख रही है । भारत या इंडिया का भी कुछ योगदान रहा होगा इसमें मुझे शंका है ।
इंडिया बनाम भारत बनाम चीन
बात जब भाषा और लिपि की हो रही हो तो इस बात का उल्लेख करना अनुचित नहीं होगा कि हम भारतीयों, या बेहतर होगा कहना इंडियन्ज, और चीनियों में गंभीर अंतर हैं । चीन के लोग कमोबेश अपनी भाषा/लिपि के प्रति गौरव रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका कार्य यथासंभव अपनी भाषा/लिपि के माध्यम से हो । इसके विपरीत हममें भाषाई गौरव का अभाव है । अपनी भाषाओं के प्रयोग से यथासंभव बचें इसकी कोशिश हम अधिक करते हैं और अंग्रेजी के पक्ष में तमाम तर्क खोज लाते हैं । चीनी सरकार तथा वहां के तकनीकी विशेषज्ञ यह अच्छी तरह से समझते आये हैं कि वहां के लोग पहले अंग्रेजी सीखें और तत्पश्चात् वे कंप्यूटर पर बैठें ऐसा विचार करके चलना मूर्खतापूर्ण होगा । चीन की सोच यह रही है कि उसकी जनता को अंग्रेजी सीखने की जहमत ही न उठानी पड़े, बल्कि उन्हें कंप्यूटर तथा इंटरनेट सुविधा उनकी भाषा – मैंडरिन – में उपलब्ध कराई जाए । आज कंप्यूटरों के क्षेत्र में जो प्रगति हो चुकी है उसके कारण भाषाएं तथा उनकी लिपियां कोई समस्या नहीं रह गयी हैं । इस तथ्य के मद्देनजर चीन ने इंफर्मेशन टेक्नालॉजी का प्रयोग अपने लोगों के लिए अधिक किया है । अपने लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज करके केवल पाश्चात्य देशों को निर्यात हेतु अंग्रेजी के माध्यम से सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कार्य होवे यह चीन को स्वीकार्य नहीं रहा ऐसा मानना है मेरा । सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में वे हमसे पीछे दिखते हैं, पर मैं समझता हूं कि वस्तुतः ऐसा है नहीं । उनकी प्राथमिकता में उसके अपने लोग शामिल रहे हैं, जिसे अपनी भाषा/लिपि में इंटरनेट सेवा चाहिए । मेरा सोचना है कि इस नीति के कारण सॉफ्टवेयर के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय बाजार से लाभ कमाने में चीन हमारे देश से पीछे रहा है । लेकिन उस कमी की भरपाई उसने हार्डवेयर के क्षेत्र में अतुलनीय प्रगति करके की है । हमारे यहां तो हार्डवेयर क्षेत्र प्रायः गायब-सा है, और साफ्टवेयर अधिकांशतः निर्यात के लिए, देशवासियों और स्वदेशी भाषाओं के लिए बहुत कम । बहरहाल मैं तो ऐसा ही मानता हूं ।
वास्तव में हमारी स्थिति चीन के ठीक उल्टी है । अपने यहां सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो रहा कार्य प्रमुखतया निर्यात के लिए रहा है और अंग्रेजी पर अपने यहां अत्यधिक जोर रहा है । यहां तक कहा जाता है कि अंग्रेजी के बल पर ही तो हम सूचना-क्षेत्र में अग्रणी और ‘धुरंधर’ होंगे । हमारी प्रथमिकता यह कभी नहीं रही कि हम स्वयं अपने देशवासियों के लिए ऐसे सॉफ्टवेयर विकसित करें कि हमारी अधिकांश जनता, जो अंग्रेजी नहीं जानती है, इंटरनेट का प्रयोग कारगर तरीके से कर सके । हमारे विशेषज्ञों का शायद ही कभी यह गंभीर प्रयास रहा हो कि अंग्रेजी में उपलब्ध जानकारी को वे अपने देशवासियों के समक्ष उनकी भाषा – जनभाषा – में प्रस्तुत करें, जैसा कि विश्व के सभी प्रमुख देशों में होता रहा है । सच पूछिए तो अपने नीति-निर्धारकों की भाषाई नीति ही दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक रही है । वे इस बात पर जोर डालते रहे हैं कि समस्त ज्ञान अंग्रेजी में है, उसे पाना है तो हर व्यक्ति स्वयं अंग्रेजी सीखे । इसे वे ‘अंग्रेजी थोपना’ नहीं मानते हैं । इसके विपरीत चीन की नीति रही है कि हर चीनी को अंग्रेजी की जरूरत नहीं । जो ज्ञान अंग्रेजी में उपलब्ध है उसे अंग्रेजी जानने वाले विशषज्ञों द्वारा उनकी भाषा – मैंडरिन – में उनके सामने रखी जाएगी । अंग्रेजी सीखने का समय- तथा श्रम-साध्य कार्य हर व्यक्ति को करना पड़े ऐसी नीति चीन की नहीं रही है । इसी सिद्धांत को लेकर चीन चला है, और उसके प्रयास रहे हैं कि किसी चीनी को लैटिन लिपि का भी ज्ञान न हो तो भी वह बखूबी इंटरनेट का उपयोग कर सके । चीन उन देशों में अग्रणी रहा है जिन्होंने लैटिन लिपि की अनिवार्यता से मुक्त होने की पुरजोर कोशिश की और अंत में सफल भी हो गया । मेरा अनुमान है कि भारत या इंडिया का इस प्रयास में कोई योगदान नहीं रहा ।
वेब साइट नाम और भारतीय लिपियां
इंटरनेट वेब साइटों के नाम और उन पर प्रस्तुत पाठ्य सामग्री का लैटिनेतर लिपियों में उपलब्ध होना अवश्य ही उन उपयोक्ताओं के लिए लाभप्रद है जो उक्त लिपि और अंग्रेजी से सुपरिचित नहीं हैं । अब सवाल उठता है कि आईसीएएनएन का निर्णय अपने देश के संदर्भ में कोई अहमियत रखता है क्या ? इस तथ्य को नहीं झुठलाया जा सकता है कि अपने देश में समाज का अपेक्षया संपन्न वर्ग ही कंप्यूटरों और इंटरनेट तक पहुंच रखता है, और अपवादों को छोड़ दें तो, यह वह वर्ग है जो अंग्रेजी भाषा में अधिक दिलचस्पी रखता है और उसी को प्राथमिकता के साथ प्रयोग में लेने का आदी है । इस वर्ग के जो लोग अपनी नेमप्लेट (नामपट्ट) तक देवनागरी या अन्य भारतीय लिपियों में लिखने से परहेज रखते हैं वे क्या लैटिनेतर लिपि में वेेब नाम चुनना चाहेंगे ? अपने शहरों में दुकानों/कार्यालयों के नामपट्ट तक चयनित तौर पर अंग्रेजी में रहते हैं; ऐसे में भारतीय लिपियों की बात कौन करेगा ? उपभोक्ता वस्तुओं के नाम और उनके साथ संलग्न जानकारी तक भारतीय लिपियों में कम ही देखने को मिलती है । देवनागरी की स्थिति तो और भी दयनीय है । बाजार में हिंदी संगीत/गानों का कैसेट खरीदें, क्या उस पर देवनागरी में लिखा दिखता है कभी ? हिंदी फिल्मों की ‘कास्टिंग’ आदि का विवरण तक देवनागरी में देखने को नहीं मिलता, तब भला उसका प्रयोग इंटरनेट वेब नामों में कौन करेगा ।
अपने देश की प्रायः सभी, विशेषकर सरकारी, वेब साइटें मूलतः अंग्रेजी में बनी हैं। कम ही स्थल हैं जिनमें हिंदी/देवनागरी में जानकारी मिलेगी । उन साइटों का ढांचा भी अक्सर अंग्रेजी में ही रहता है, केवल पाठ्य हिंदी में देखने को मिलेगा । प्रयोग में लिए जा रहे ‘आइकॉन’ और ‘बटन’ पर लैटिन वर्ण ही झलकते हैं । चाहे बैंकीय लेन-देन हो या रेलवे आरक्षण, अथवा इंटरनेट पर सरकारी-गैरसरकारी फार्म भरना, सभी कुछ अंग्रेजी में रहता है । तब आईसीएएनएन का उक्त निर्णय भारत के संदर्भ में क्या कोई माने रखता है । शायद नहीं !
और बात खत्म करते-करते आंरभ में उल्लिखित वेब साइट Sun0769 के एक पेज की तस्वीर पेश कर दूं, यह दर्शाने के लिए कि लैटिनेतर लिपि के प्रयोग का क्या मतलब है ।

आगे है ‘गूगल अनुवादक’ से प्राप्त वही पृष्ठ । मुझे लगता है कि गूगल अनुवादक हिंदी की तुलना में चीनी भाषा के लिए अधिक सफल है । इस मामले में भी वे हमसे आगे हैं ।

और अंत में यह देखिए तोक्यो विश्वविद्यालय का एक वेब पेज

क्या अपने देश में कोई विश्वविद्यालय है जिसकी वेब साइट पर भारतीय लिपि भी दिखती हो ? मेरी जानकारी में नहीं ! – योगेन्द्र जोशी
‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ और राजभाषा हिंदीं
अक्टूबर 13, 2009
अगले वर्ष इसी माह (3 से 14 अक्टूबर, 2010) अपने देश, ‘इंडिया’, में ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ (जिन्हें हिंदी में शायद राष्ट्रकुल खेल कहा जाता है) का ‘भव्य’ आयोजन होना है । मेरी शुभकामनाएं आयोजकों के प्रति कि उन्हें इस आयोजन में पूर्ण सफलता मिले तथा वे देश की ‘दांव पर लगी प्रतिष्ठा’ को बचाने में कामयाब रहें । उक्त खेल उत्कंठित देशवासियों तथा उत्सुक खेलप्रेमियों की आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं के अनुकूल संपन्न होवें यह मेरी दैवी शक्तियों से प्रार्थना है । (आयोजकों की वेबसाइटः http://www.cwgdelhi2010.org/home.aspx)
 समाचार माध्यमों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि उक्त आयोजन की तैयारियां संतोषजनक नहीं चल रही हैं । खैर तैयारी के बारे में कुछ कह पाना शायद आम नागरिक के लिए संभव नहीं । लेकिन एक बात पर टिप्पणी करने का मेरा भी मन हो आया, जब मेरी नजर संबंधित ‘लोगो’ (क्या कहते हैं इसे, प्रतीकचिह्न ?) पर पड़ी, जिसे यहां इन शब्दों के साथ छाप रहा हूं । मेरी जानकारी में ‘हिंदी’ राजभाषा है, और देवनागरी, न कि रोमन, उसकी लिपि है । मेरे अनुमान से अपने देश की सरकार इस राजभाषा को स्थान देती है, कम से कम मुद्रित सामग्री में । अगर सरकार से पूछा जाय तो यही सुनने को मिलेगा कि राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है और उसे बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं । अगर स्थान नहीं देगी तो राजभाषा किस काम की रह जायेगी भला ? किंतु ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ के लिए जो ‘लोगो’ (logo) प्रयोग में लिया जा रहा है उसमें कहीं एक भी अक्षर देवनागरी का नहीं है, जैसा पहले चित्र से जाहिर है | क्या इस लोगो में अंग्रेजी के साथ देवनागरी में भी वांछित शब्दों का उल्लेख नहीं होना चाहिए था ? लोगो क्या वैसा नहीं हो सकता था जैसा मेरे द्वारा संशोधित दूसरे चित्र में दिखाया गया है ? ऐसा ही कुछ संभव था और है । क्या वजह है कि आयोजकों को राजभाषा से इतना परहेज है ? क्या वजह है कि सरकार राजभाषा के प्रति इतना उदासीन है, लेकिन फिर भी उसे ‘राजभाषा’ खिताब से वंचित करने पर विचार नहीं करती ?
समाचार माध्यमों में छपी खबरों से ऐसा लगता है कि उक्त आयोजन की तैयारियां संतोषजनक नहीं चल रही हैं । खैर तैयारी के बारे में कुछ कह पाना शायद आम नागरिक के लिए संभव नहीं । लेकिन एक बात पर टिप्पणी करने का मेरा भी मन हो आया, जब मेरी नजर संबंधित ‘लोगो’ (क्या कहते हैं इसे, प्रतीकचिह्न ?) पर पड़ी, जिसे यहां इन शब्दों के साथ छाप रहा हूं । मेरी जानकारी में ‘हिंदी’ राजभाषा है, और देवनागरी, न कि रोमन, उसकी लिपि है । मेरे अनुमान से अपने देश की सरकार इस राजभाषा को स्थान देती है, कम से कम मुद्रित सामग्री में । अगर सरकार से पूछा जाय तो यही सुनने को मिलेगा कि राजभाषा का प्रयोग अधिकाधिक हो रहा है और उसे बढ़ावा देने के लिए तमाम कोशिशें जारी हैं । अगर स्थान नहीं देगी तो राजभाषा किस काम की रह जायेगी भला ? किंतु ‘कॉमनवेल्थ गेम्ज’ के लिए जो ‘लोगो’ (logo) प्रयोग में लिया जा रहा है उसमें कहीं एक भी अक्षर देवनागरी का नहीं है, जैसा पहले चित्र से जाहिर है | क्या इस लोगो में अंग्रेजी के साथ देवनागरी में भी वांछित शब्दों का उल्लेख नहीं होना चाहिए था ? लोगो क्या वैसा नहीं हो सकता था जैसा मेरे द्वारा संशोधित दूसरे चित्र में दिखाया गया है ? ऐसा ही कुछ संभव था और है । क्या वजह है कि आयोजकों को राजभाषा से इतना परहेज है ? क्या वजह है कि सरकार राजभाषा के प्रति इतना उदासीन है, लेकिन फिर भी उसे ‘राजभाषा’ खिताब से वंचित करने पर विचार नहीं करती ? 
लोगो में अंकित शब्द वास्तव में प्रथमतः राजभाषा में और तत्पश्चात् उसके साथ अंग्रेजी में होने चाहिए थे, क्योंकि संविधान के अनुसार हिंदी (देवनागरी लिपि में) प्रमुख राजभाषा है और अंग्रेजी उसकी सहायक राजभाषा । सरकारी तंत्र ने घोषित सांविधानिक नीति के विरुद्ध अंग्रेजी को प्रमुख राजभाषा का दर्जा दे रखा है । फिर भी घोषित राजभाषा अंग्रेजी की सहायक राजभाषा के तौर पर तो प्रयुक्त हो ही सकती है । राजभाषा हिंदी के प्रति इतना भी सम्मान अथवा सदाशयता नीतिनिर्धारकों के मन में क्यों नहीं है कि थोड़ा बहुत रस्मअदायगी ही निभा लें ?
एक और बात मेरे जेहन में उठती है । विश्व के अन्य प्रमुख देश खेल और तत्सदृश कोई और आयोजन करते हैं तो पूरी कार्यवाही अंग्रेजी के अतिरिक्त अपनी भाषा में भी प्रस्तुत करते हैं । याद किजिए जब चीन में ओलंपिक खेल संपन्न हुए थे । अपने देश में क्या होगा ? क्या उक्त खेलों के अवसर पर कहीं देवनागरी लिखी देखने को मिलेगी ? कहीं हिंदी लफ़्ज़ सुनने को मिलेंगे ? मुझे शंका है कि उस मौके पर भी अपनी राजभाषा सदा की तरह तिरस्कृत ही रहेगी ।
मुझे अंग्रेजी के प्रयोग पर आपत्ति नहीं है । विश्व में अन्य देश भी इसको महत्त्व दे रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कि अपनी मौलिक भाषाओं को ही भूल जाएं । प्रमुख देशों में कोई ऐसा नहीं होगा जहां अपने देश की भाषा को शासित प्रजा की भाषा के तौर पर देखा जाता हो और अंग्रेजी को शासकों की भाषा बने रहने दिया जा रहा हो । देश में दो प्रकार की भाषाएं हैं, एक आम जन की देसी भाषाएं और दूसरे अंग्रेजी जो आज भी देश पर राज करने वालों की भाषा है, ठीक वैसे ही जैसे विदेशी राज में था । राजनीतिक तौर पर स्वतंत्र होने के बावजूद इस देश का शासक वर्ग स्वयं को आम जनता से ऊपर मानता है और अपने को उनसे अलग रखने के लिए अंग्रेजी का हथियार इस्तेमाल करता आ रहा है । क्या ऐसी मानसिकता वाले शासकों से यह देश कभी मुक्त हो सकेगा ? शायद कभी नहीं ! – योगेन्द्र जोशी
14 सितंबर, हिंदी दिवस – रस्मअदायगी का एक दिन, हर बीते वर्ष की भांति
सितम्बर 14, 2009
आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर ।
सर्वप्रथम मैं हिंदी-प्रमियों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि उनका भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव बना रहे और यह भी कि वे अपने भाषाई प्रयासों में सफल होवें ।
तारीख के हिसाब से कोई 60 साल पहले आज ही के दिन देश में सर्वाधिक बोली/समझी जाने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा की उपाधि दी गयी थी । रस्मअदायगी के तौर पर इस दिन उच्चपदस्थ लोग, चाहे वे राजनीति में हों या प्रशासन में अथवा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में, यह कहते हुए सुने जाएंगे कि हमें राजभाषा हिन्दी अपनानी चाहिए । किसको अपनानी चाहिए हिंदी और किस क्षेत्र में और किस रूप में यह वह स्पष्ट नहीं कहते हैं । ऐसा लगता है कि वे आम आदमी को नसीहत देना चाहते हैं कि वह हिंदी को यथासंभव अधिकाधिक इस्तेमाल में ले । लेकिन वे स्वयं इसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहते हैं और अंगरेजी के सापेक्ष वस्तुस्थिति को यथावत् बनाये रखने के पक्षधर हैं ।
हिंदी के राजभाषा बनाए जाने के औचित्य पर मुझे सदा ही शंका रही है । सैद्धांतिक तौर पर हिंदी के पक्ष में आरंभ में जो तर्क दिये गये थे वे निराधार तथा असत्य थे यह मैं नहीं कहता । किंतु तथ्यात्मक तर्क ही पर्याप्त नहीं माने जा सकते हैं । वास्तविकता के धरातल पर वे तर्क स्वीकार किये जा रहे हैं या नहीं, हामी भर लेने के बावजूद उनके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोग रुचि लेते हैं या नहीं जैसी बातें अधिक महत्त्व रखते हैं । अपनी बात मैं यूं स्पष्ट करता हूं: आप सिगरेट के किसी लती को सलाह दें कि उसका धूम्रपान करना नुकसानदेह है और वह आपकी बात मानते हुए कहे कि ‘लेकिन मैं फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता’ तो आप क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि कोई न कोई रास्ता तो खोजा ही जाना चाहिए । एक व्यक्ति को रास्ते पर लाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाये जा सकते हैं, समझाया-बुझाया जा सकता है, जोर-जबरदस्ती की जा सकती है, डराया-धमकाया जा सकता है, इत्यादि, और अंततः सफलता मिल भी सकती है । किंतु ऐसा कोई रास्ता समूचे देश के लिए संभव नहीं है । किसी दिशा में अग्रसर होने की सन्मति यदि लोगों में आ जाये तो ठीक, अन्यथा सब भगवान् भरोसे । राजभाषा हिंदी के मामले में स्थिति कुछ ऐसी ही है ।
यदि अपने देशवासी किसी न किसी बहाने अंगरेजी का प्रयोग यथावत् बनाये रखना चाहें तो फिर इस राजभाषा का अर्थ ही क्या है ? जब मैं अपने देश की तुलना विश्व के अन्य प्रमुख देशों से करता हूं तो पाता हूं कि अपना देश है ही विचित्र, सबसे अजूबा, विरोधाभासों और विसंगतियों से परिपूर्ण । यह विचित्रता सर्वत्र व्याप्त है, किंतु यहा पर इसका उल्लेख अपनी देसी भाषाओं के संदर्भ में ही कर रहा हूं । हम यह मानते है कि हमारी भाषाएं सुसंपन्न हैं, किंतु उन्हें लिखित रूप में प्रयोग में न लेकर केवल बोले जाने तक सीमित रखना चाहते हैं । क्यों ? इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास नहीं, कदाचित् एक प्रकार का जड़त्व हमें घेरे हुए है कि सार्थक परिवर्तन करने को हम उत्सुक और प्रयत्नशील नहीं हैं, न ऐसा होना चाहते हैं ।
इसमें दो राय नहीं है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रायः सर्वत्र हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं ही बोली जाती हैं, चाहे बाजार में खरीद-फरोख्त का काम हो या पड़ोसी के हालचाल पूछने का या फोन पर किसी नाते-रिस्तेदार से बात करने का । यहां तक कि अंगरेजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे भी स्कूल आते-जाते परस्पर अपनी देसी भाषा में ही बोलते दिखते हैं । कार्यालयों में अधिकांशतः सभी स्थानीय भाषा में ही सामान्य वार्तालाप करते हुए पाये जायेंगे । अपवादों को छोड़ दें । राजनीतिक क्षेत्र में तो जनता के सामने बातें क्षेत्रीय भाषाओं में ही रखी जाती हैं । किंतु जैसे ही कहीं कोई औपचारिक बात हो, हम तुरंत ही अंगरेजी में उतर आते हैं । अपनी बात स्थानीय भाषा में कहेंगे जरूर, किंतु उसी को जब लिखित रूप में व्यक्त करना हो तो अंगरेजी हमारी प्राथमिकता बन जाती है । तब हिंदी या अन्य देसी भाषा का प्रयोग समाज के निम्नतम वर्ग या अंगरेजी न पढ़े-लिखे लोगों तक रह जाता है । जिसको थोड़ी भी अंगरेजी आती है वह अपनी भाषाओं में लिखकर कुछ कहने को तैयार नहीं । चाहे रेलयात्रा का आरक्षण हो या बैंकों में कारोबार करने का या अपने ही क्षेत्र का पता चिट्ठी पर लिखने का, सर्वत्र अंगरेजी ही देखने को मिलेती है, कुछ अपवादों को छोड़कर ।
निःसंदेह बोलचाल में हिंदी का प्रयोग देश भर में बढ़ा है । देश के किसी कोने में जाइये रिक्शा-ऑटों वालों से, चाय वालों से, सामान्य दर्जे के होटल वालों से हिंदी में बात करना अधिक सुविधाजनक सिद्ध होता है ऐसा मैंने देशाटन में अनुभव किया है । किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी लिखित रूप में हिंदी शायद ही कहीं दिखाई देती है । सभी सार्थक जानकारी अंगरेजी में ही लिखित आपको मिलेगी भले ही जनसामान्य के उस जानकारी का हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होना अधिक लाभप्रद क्यों न हो । मैं उदाहरण पेश करता हूं । मेरी बातें मुख्यतः हिंदीभाषी क्षेत्रों पर लागू होती हैं ।
हम हिंदुस्तानियों का अंग्रेजी-मोह अद्वितीय और तारीफे-काबिल है । आम पढ़े-लिखे हिंदुस्तानी की दिली चाहत रहती है वह इतनी अंगरेजी सीख ले कि उसमें बिला रुकावट गिटिर-पिटिर कर सके और दूसरों को प्रभावित कर सके । अंगरेजी की खातिर विरासत में मिली अपनी मातृभाषा की अनदेखी करना भी उसे मंजूर रहता है । लेकिन सब कुछ करने के बावजूद कोई न कोई कमी रह ही जाती है । यह कमी कभी-कभी उच्चारण के स्तर पर साफ नजर आ जाती है । पत्रकारिता से जुड़े लोगों के मामले में यह कमी तब नजर में आ जाती है जब उन्हें अंगरेजी में उपलब्ध समाचार की हिन्दी अनुवाद करते हुए कुछ अंगरेजी शब्दों को देवनागरी में लिखना पड़ता है । आगे के चित्र में ऐसे दो दृष्टांत पेश हैं:

गौर करें कि ऊपर दिये चित्र में अंगरेजी के दो शब्दों, ‘याचिंग’ एवं ‘वोग्यू’, को त्रुटिपूर्ण उच्चारण के अनुरूप देवनागरी में लिखा गया है । माथापच्ची करने पर मुझे एहसास हुआ कि ‘याचिंग’ वस्तुतः ‘यौटिंग (या यॉटिंग?)’ के लिए लिखा गया है जिसकी वर्तनी (स्पेलिंङ्) YACHTING होती हैं । YACHT वस्तुतः ‘पालदार या ऐसी ही शौकिया खेने के लिए बनी नाव को कहा जाता है । तदनुसार YACHTING संबंधित नौकादौड़ में भाग लेने का खेल होता है । जिस व्यक्ति ने इस शब्द का सही उच्चारण न सुना हो (रोजमर्रा की बातचीत में इसका प्रयोग ही कितना होगा भला!) और शब्दकोश की मदद न ली हो, वह इसे यदि ‘याचिंग’ उच्चारित करे तो आश्चर्य नहीं है । यह उच्चारण बड़ा स्वाभाविक लगता है । पर क्या करें, अंगरेजी कभी-कभी इस मामले में बड़ा धोखा दे जाती है ।
और दूसरा शब्द है ‘वोग्यू’ । समाचार से संबंधित चित्र में जो पत्रिका दृष्टिगोचर होती है उसका नाम है VOGUE नजर आता है । यह अंगरेजी शब्द है जिसका उच्चारण है ‘वोग’ और अर्थ है ‘आम प्रचलन में’, ‘व्यवहार में सामान्यतः प्रयुक्त’, ‘जिसका चलन अक्सर देखने में आता है’, इत्यादि । अपने स्वयं के अर्थ के विपरीत VOGUE प्रचलन में अधिक नहीं दिखता और कदाचित् अधिक जन इससे परिचित नहीं हैं । मैंने अपने मस्तिष्क पर जोर डालते हुए उन शब्दों का स्मरण करने का प्रयास किया जो वर्तनी के मामले में मिलते-जुलते हैं । मेरे ध्यान में ये शब्द आ रहे हैं (और भी कई होंगे):
argue, dengue, demagogue, epilogue, intrigue, league, prologue, rogue, synagogue, The Hague (नीदरलैंड का एक नगर), tongue.
इनमें से पहला, argue (बहस करना), एवं अंतिम, tongue (जीभ), सर्वाधिक परिचित शब्द हैं ऐसा मेरा अनुमान है । और दोनों के उच्चारण में पर्याप्त असमानता है । पहला ‘आर्ग्यू’ है तो दूसरा ‘टङ्’ । अतः बहुत संभव है कि मिलते-जुलते वर्तनी वाले अपरिचित नये शब्द का उच्चारण कोई पहले तो कोई अन्य दूसरे के अनुसार करे । उक्त उदाहरण में संभव है कि संवाददाता ‘आर्ग्यू’ से प्रेरित हुआ हो । समता के आधार पर उच्चारण का अनुमान अंगरेजी में अ संयोग से स्वीकार्य हो सकता है । सच कहूं तो argue की तरह का कोई शब्द मेरी स्मृति में नहीं आ रहा है । ध्यान दें कि सूची में दिये गये शब्द dengue (मच्छरों द्वारा फैलने वाला एक संक्रमण) का भी उच्चारण शब्दकोश ‘डेंगे’ बताते हैं, न कि ‘डेंग्यू’ या ‘डेंङ्’ । सूची के अन्य सभी के उच्चारण में परस्पर समानता है और वे इन दो शब्दों से भिन्न हैं ।
‘याचिंग’ तथा ‘वोग्यू’ टाइपिंग जैसी किसी त्रुटि के कारण गलती से लिख गये हों ऐसा मैं नहीं मानता । वास्तव में इस प्रकार के कई वाकये मेरे नजर में आते रहे हैं । हिंदी अखबारों में मैंने आर्चीव (archive आर्काइव के लिए), च्यू (chew चो), कूप (coup कू), डेब्रिस (debris डेब्री), घोस्ट (ghost गोस्ट), हैप्पी (happy हैपी), हेल्दी (healthy हेल्थी), आइरन (iron आयर्न), जिओपार्डाइज (jeopardize ज्येपार्डाइज ), ज्वैल (jewel ज्यूल), लाइसेस्टर (Leicester लेस्टर शहर), लियोपार्ड (leopard लेपर्ड), ओवन (oven अवन), सैलिस्बरी (Salisbury सॉल्सबरी शहर), सीजोफ्रीनिआ (schizophrenia स्कित्सफ्रीनिअ), आदि ।
दोषपूर्ण उच्चारण के अनुसार देवनागरी में लिखित शब्दों के पीछे क्या कारण हैं इस पर विचार किया जााना चाहिए । मेरा अनुमान है कि हिंदी पत्रकारिता में कार्यरत लोगों की हिंदी तथा अंगरेजी, दोनों ही, अव्वल दर्जे की हो ऐसा कम ही होता है । अपने देश में बहुत से समाचार तथा उन्नत दर्जे की अन्य जानकारी मूल रूप में अंगरेजी में ही उपलब्ध रहते हैं । मौखिक तौर पर बातें भले ही हिंदी में भी कही जाती हों, किंतु दस्तावेजी तौर पर तो प्रायः सभी कुछ अंगरेजी में रहता है । ऐसे में हिंदी पत्रकार अनुवाद के माध्यम से ही संबंधित जानकारी हिंदी माध्यमों पर उपलब्ध कराते हैं । व्याकरण के स्तर पर अच्छी अंगरेजी जानने वाले का उच्चारण ज्ञान भी अच्छा हो यह आवश्यक नहीं है, क्योंकि अंगरेजी में उच्चारण सीखना अपने आप में अतिरिक्त प्रयास की बात होती है । अतः समुचित अध्ययन के अभाव में त्रुटि की संभावना अंगरेजी में कम नहीं होती । तब अंगरेजी शब्द VOGUE एवं YACHTING का देवनागरी में क्रमशः ‘वोग्यू’ तथा ‘याचिंग’ लिखा जाना असामान्य बात नहीं रह जाती है ।
मेरी बातें किस हद तक सही हैं यह तो हिंदी पत्रकारिता में संलग्न जन ही ठीक-ठीक बता सकते हैं, अगर इस प्रयोजन से उन्होंने कभी अपने व्यवसाय पर दृष्टि डाली हो तो । अंगरेजी में उच्चारण सीखना कठिन कार्य है इसकी चर्चा मुझे करनी है । इस बात पर मैं जोर डालना चाहता हूं कि वर्तनी-साम्य देखकर उच्चारण का अनुमान लगाना अंगरेजी में असफल हो सकता है । अपने मत की सोदाहरण चर्चा अगली पोस्टों में मैं जारी रखूंगा । – योगेन्द्र