14 सितंबर, हिंदी दिवस – रस्मअदायगी का एक दिन, हर बीते वर्ष की भांति
सितम्बर 14, 2009
आज हिंदी दिवस है, 14 सितंबर ।
सर्वप्रथम मैं हिंदी-प्रमियों के प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं कि उनका भारतीय भाषाओं के प्रति लगाव बना रहे और यह भी कि वे अपने भाषाई प्रयासों में सफल होवें ।
तारीख के हिसाब से कोई 60 साल पहले आज ही के दिन देश में सर्वाधिक बोली/समझी जाने वाली भाषा हिंदी को राजभाषा की उपाधि दी गयी थी । रस्मअदायगी के तौर पर इस दिन उच्चपदस्थ लोग, चाहे वे राजनीति में हों या प्रशासन में अथवा अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में, यह कहते हुए सुने जाएंगे कि हमें राजभाषा हिन्दी अपनानी चाहिए । किसको अपनानी चाहिए हिंदी और किस क्षेत्र में और किस रूप में यह वह स्पष्ट नहीं कहते हैं । ऐसा लगता है कि वे आम आदमी को नसीहत देना चाहते हैं कि वह हिंदी को यथासंभव अधिकाधिक इस्तेमाल में ले । लेकिन वे स्वयं इसके इस्तेमाल की जिम्मेदारी से मुक्त रहना चाहते हैं और अंगरेजी के सापेक्ष वस्तुस्थिति को यथावत् बनाये रखने के पक्षधर हैं ।
हिंदी के राजभाषा बनाए जाने के औचित्य पर मुझे सदा ही शंका रही है । सैद्धांतिक तौर पर हिंदी के पक्ष में आरंभ में जो तर्क दिये गये थे वे निराधार तथा असत्य थे यह मैं नहीं कहता । किंतु तथ्यात्मक तर्क ही पर्याप्त नहीं माने जा सकते हैं । वास्तविकता के धरातल पर वे तर्क स्वीकार किये जा रहे हैं या नहीं, हामी भर लेने के बावजूद उनके अनुरूप कार्य हो रहा है कि नहीं, नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार लोग रुचि लेते हैं या नहीं जैसी बातें अधिक महत्त्व रखते हैं । अपनी बात मैं यूं स्पष्ट करता हूं: आप सिगरेट के किसी लती को सलाह दें कि उसका धूम्रपान करना नुकसानदेह है और वह आपकी बात मानते हुए कहे कि ‘लेकिन मैं फिर भी सिगरेट पीना नहीं छोड़ सकता’ तो आप क्या करेंगे ? आप कहेंगे कि कोई न कोई रास्ता तो खोजा ही जाना चाहिए । एक व्यक्ति को रास्ते पर लाने के लिए तरह-तरह के नुस्खे अपनाये जा सकते हैं, समझाया-बुझाया जा सकता है, जोर-जबरदस्ती की जा सकती है, डराया-धमकाया जा सकता है, इत्यादि, और अंततः सफलता मिल भी सकती है । किंतु ऐसा कोई रास्ता समूचे देश के लिए संभव नहीं है । किसी दिशा में अग्रसर होने की सन्मति यदि लोगों में आ जाये तो ठीक, अन्यथा सब भगवान् भरोसे । राजभाषा हिंदी के मामले में स्थिति कुछ ऐसी ही है ।
यदि अपने देशवासी किसी न किसी बहाने अंगरेजी का प्रयोग यथावत् बनाये रखना चाहें तो फिर इस राजभाषा का अर्थ ही क्या है ? जब मैं अपने देश की तुलना विश्व के अन्य प्रमुख देशों से करता हूं तो पाता हूं कि अपना देश है ही विचित्र, सबसे अजूबा, विरोधाभासों और विसंगतियों से परिपूर्ण । यह विचित्रता सर्वत्र व्याप्त है, किंतु यहा पर इसका उल्लेख अपनी देसी भाषाओं के संदर्भ में ही कर रहा हूं । हम यह मानते है कि हमारी भाषाएं सुसंपन्न हैं, किंतु उन्हें लिखित रूप में प्रयोग में न लेकर केवल बोले जाने तक सीमित रखना चाहते हैं । क्यों ? इसका संतोषप्रद उत्तर किसी के पास नहीं, कदाचित् एक प्रकार का जड़त्व हमें घेरे हुए है कि सार्थक परिवर्तन करने को हम उत्सुक और प्रयत्नशील नहीं हैं, न ऐसा होना चाहते हैं ।
इसमें दो राय नहीं है कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रायः सर्वत्र हिंदी अथवा अन्य क्षेत्रीय भाषाएं ही बोली जाती हैं, चाहे बाजार में खरीद-फरोख्त का काम हो या पड़ोसी के हालचाल पूछने का या फोन पर किसी नाते-रिस्तेदार से बात करने का । यहां तक कि अंगरेजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे भी स्कूल आते-जाते परस्पर अपनी देसी भाषा में ही बोलते दिखते हैं । कार्यालयों में अधिकांशतः सभी स्थानीय भाषा में ही सामान्य वार्तालाप करते हुए पाये जायेंगे । अपवादों को छोड़ दें । राजनीतिक क्षेत्र में तो जनता के सामने बातें क्षेत्रीय भाषाओं में ही रखी जाती हैं । किंतु जैसे ही कहीं कोई औपचारिक बात हो, हम तुरंत ही अंगरेजी में उतर आते हैं । अपनी बात स्थानीय भाषा में कहेंगे जरूर, किंतु उसी को जब लिखित रूप में व्यक्त करना हो तो अंगरेजी हमारी प्राथमिकता बन जाती है । तब हिंदी या अन्य देसी भाषा का प्रयोग समाज के निम्नतम वर्ग या अंगरेजी न पढ़े-लिखे लोगों तक रह जाता है । जिसको थोड़ी भी अंगरेजी आती है वह अपनी भाषाओं में लिखकर कुछ कहने को तैयार नहीं । चाहे रेलयात्रा का आरक्षण हो या बैंकों में कारोबार करने का या अपने ही क्षेत्र का पता चिट्ठी पर लिखने का, सर्वत्र अंगरेजी ही देखने को मिलेती है, कुछ अपवादों को छोड़कर ।
निःसंदेह बोलचाल में हिंदी का प्रयोग देश भर में बढ़ा है । देश के किसी कोने में जाइये रिक्शा-ऑटों वालों से, चाय वालों से, सामान्य दर्जे के होटल वालों से हिंदी में बात करना अधिक सुविधाजनक सिद्ध होता है ऐसा मैंने देशाटन में अनुभव किया है । किंतु इतना सब कुछ होते हुए भी लिखित रूप में हिंदी शायद ही कहीं दिखाई देती है । सभी सार्थक जानकारी अंगरेजी में ही लिखित आपको मिलेगी भले ही जनसामान्य के उस जानकारी का हिंदी अथवा क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होना अधिक लाभप्रद क्यों न हो । मैं उदाहरण पेश करता हूं । मेरी बातें मुख्यतः हिंदीभाषी क्षेत्रों पर लागू होती हैं ।
(1) हिंदीभाषी क्षेत्रों के प्रमुख शहरों के नामपट्टों को देखिए, अंगरेजी में मिलेंगे भले ही वहां आने-जाने वाले लोगों में अंगरेजी जानने वाले कम और हिंदी जानने वाले अधिक हों । होटलों, ‘मॉलों’ ने तो जैसे कसम खा रखी है हिंदी में न लिखने की । हिंदीभाषी क्षेत्र फिर भी हिंदी में नामोल्लेख नहीं, किस मानसिकता का द्योतक है यह ?
(2) दुकानों पर जाइए खरीद की रसीद आपको आम तौर पर अंगरेजी में ही मिलेगी । हिंदी में या हिंदी-अंगरेजी में क्यों नहीं रहती ?
(3) उपभोक्ता सामान पर नजर डालें तो उस पर लिखित सूचना आपको अंगरेजी में ही मिलेगी । बिस्कुट पैकेट हो या खाद्य तेल की बोतल या क्रीम-पेस्ट की डिबिया, कहीं हिंदी में भी लिखा मिलता है ? यह सब तब जब कि अंगरेजी के बदले हिंदी ठीक से समझने वालों की संख्या कहीं अधिक रहती है । मुझे तो इस देश के लोगों पर तब तरस आता है जब में देखता हूं कि अंगरेजी के ज्ञान से वंचित श्रमिक वर्गों के लोगों के लिए भी जानकारी अंगरेजी में ही रहती है । आप पेंट उद्योग का उदाहरण ले लें । पेंट कहां, कितना और कैसे इस्तेमाल करना है, उसके साथ क्या सावधानियां बरतनी है, आदि की बातें अंगरेजी में ही मुद्रित रहती हंै । प्रयोग में लेने वाला व्यक्ति साधारण पुताईकर्मी होता है जो आम तौर पर उसे पढ़-समझ नहीं सकता । वांछित जानकारी हिंदी या क्षेत्रीय भाषा में हो तो अधिक उपयोगी नहीं होगी क्या ? उद्योग-जगत् भूल जाता है कि ऐसे श्रमिक अंगरेजी स्कूलों में पढ़कर नहीं आते हैं; उन्हें क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान होता है बस । लेकिन कोई समझे तब न ! पर यह देश ही विचित्र है !
(4) आधुनिक जीवन की सुख-सुविधाओं के आधार रूप में उपलब्ध उपस्करों/उपकरणों, यथा टेलीविजन, फ्रिज, ऐसी, वाशिंग मशीन या कार-स्कुटर, के साथ उपलब्ध दिशा-निर्देश पुस्तिकाओं पर अगर गौर करें तो पाएंगे कि वे सामान्यतः अंगरेजी में ही लिखे रहते हैं । व्यापारिक संस्थाओं के लिए इस तथ्य का कोई अर्थ नहीं है कि अंगरेजी तो इस देश की 10 प्रतिशत जनता को भी नहीं आती । क्या उन्हें हिंदी तथा अन्य भाषाओं में जानकारी नहीं देनी चाहिए ?
(5) आप चिकित्सक से परामर्श लें तो वह दवा और हिदायतें अंगरेजी में लिखेगा, बिना यह सोचे-समझे कि मरीज अंगरेजी जानता भी है कि नहीं । सब बातचीत हिंदी या स्थानीय भाषा में होगी, पर लिखित निर्देश ? हिंदी या अन्य भाषा स्वीकार्य नहीं ! और दवा की दुकान में जायें तो दवा की जानकारी किसी भी भारतीय भाषा में नहीं । दिलचस्प तो यह है कि तीनएक वर्ष पूर्व तत्कालीन केंद्रीय रसायन/उर्वरक मंत्री ने दवा कंपनियों के लिए आदेश पारित किया था कि वे दवा के रैपर पर नाम, निर्माण तिथि आदि की जानकारी हिंदी में भी मुद्रित करें । उस आदेश का जिक्र मैंने अन्यत्र (क्लिक करें) किया है । वह आज तक कागजी ही बना हुआ है । राजभाषा के प्रति यह रवैया ? तो राजभाषा का औचित्य क्या रहा ?
(6) हमारी सरकारों की दोहरी शिक्षा नीति भी अंगरेजी के पक्ष में खड़ी है । समाज में जो संपन्न है उसके लिए अंगरेजी स्कूल और समाज के विपन्न वर्ग के लिए क्षेत्रीय भाषा के स्कूल । यह खुलकर कहा जाता है कि अंगरेजी-विहीन स्कूली शिक्षा निरर्थक है । रोजी-रोटी सब अंगरेजी ज्ञान पर आधारित । आज हालात यह हैं कि हर व्यक्ति अपने बच्चों के लिए अंगरेजी स्कूलों की ओर दौड़ रहा है । गली-कूचों में नये-नये ‘अंगरेजी मीडियम’ स्कूल खुल रहे हैं और देसी भाषाओं वाले स्कूल बेकार सिद्ध हो रहे हैं । हालात यह हैं कि वहां के बच्चे प्राथमिक शिक्षा के बाद भी अपना नाम नहीं लिख-पढ़ सकते । ऐसे में अपनी राजभाषा की अहमियत ही क्या रह जाती है । और मुद्देे का सबसे दुःखद पहलू तो यह है कि गैर-अंगरेजी स्कूली के बच्चे भाषाई कुंठा के शिकार हो रहे हैं । जब राजभाषा की हालत ऐसी हो तो उसकी सार्थकता क्या रह जाती है ?
(7) हिंदी की लिपि देवनागरी है न कि रोमन । हिंदी और देवनागरी के बीच का संबंध बहुत पुराना है और यह लिपि मूलतः संस्कृत और तदनुसार हिंदी की ध्वनियों के अनुरूप ढली हुई है । रोमन लिपि उसका स्थान नहीं ले सकती है । फिर भी आजकल हिंदी को रोमन लिपि में लिखने का चलन देखने में आ रहा है । लिपि के मामले में तो हिंदी की स्थिति अन्य भारतीय भाषाओं से भी बदतर हो चली है । आप बाजार में हिंदी संगीत के कैसेट/सीडी खरीदने चलिए, कैसेट पर लिखित जानकारी विशुद्ध अंगरेजी में मिलेगी । पता नहीं क्यों संबंधित औद्योगिक संस्थानों को देवनागरी से इतनी नफरत है ?
(8) और यही हाल सिने-जगत् के चलचित्रों तथा टेलीविजन चैनलों के कार्यक्रमों का है । फिल्में/धारावाहिक हिंदी के होते हैं लेकिन निर्माता-निर्देशक-कलाकारों आदि की जानकारी रोमन/अंगरेजी में मिलेगी । इतना अनर्थ तो तमिल, तेलुगू, बांग्ला आदि के साथ भी नहीं होता । विज्ञापनों में तो रोमन में लिखित हिंदी आम बात हो गयी है । ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न मीडिया के लोग हिंदी के शब्दों को अंगरेजी शब्दों और उसकी लिपि को रोमन से विस्थापित करने का संकल्प ले चुके हैं । हिंदी के साथ हर प्रकार की छेड़छाड़ करने की पूरी छूट मानों उनको मिली हुई है । लिपि के साथ कितनी ज्यादती हो रही है इस पर एक वार्ता कल (13 सितंबर) के ‘याहू-जागरण अंतरजाल-समाचार’ (क्लिक करें) पर मुझे पढ़ने को मिला था ।
(9) यह सभी स्वीकारते हैं हिंदी विश्व में सर्वाधिक बोली-समझी जाने वाली 3-4 भाषाओं में से एक है । कुछ लोग इसे संयुक्त राष्ट्र संगठन (यू एन ओ) की सातवीं आधिकारिक भाषा का दर्जा दिलाने की बात करते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि अपने ही घर में वह राजभाषा की उपाधि के बावजूद अप्रयुक्त चल रही है । व्यावसायिक लाभ की संभावनाओं के मद्देनजर गूगल, याहू जैसी संस्थाएं हिंदी को स्थान दे रही हैं, किंतु हकीकत यह है कि व्यावसायिक संस्थान इसे वह सम्मान नहीं देते हैं जो वे अन्य कई भाषाओं को देते हैं जिनके बोलने-जानने वाले मुश्किल से एक-दो करोड़ या उससे भी कम है । अंतरराष्ट्रीय बाजार में कंप्यूटर, प्रिंटर, कैमरा आदि के साथ यूनानी, तुर्की, अरबी, हेब्रू, आदि भाषाओं में मुद्रित निर्देश-पुस्तिका की उम्मीद की जा सकती है, किंतु हिंदी में नहीं । वे जानते हैं कि देश में निर्मित उपभोक्ता वस्तुओं के संदर्भ में ही जब हिंदी का महत्त्व नहीं तो वे क्यों हिंदी प्रयोग में लें ।
(10) जमाना अंतरजाल का है और वेबसाइटें जानकारी के स्रोत बनते जा रहे हैं । हर देश में अपनी भाषाओं में बेवसाइटें विकसित की जा रही हैं । अपने देश में भी सरकारी स्तर पर हिंदी में भी वेबसाइटों की औपचारिकता निभाई जा रही है, किंतु वे अंगरेजी में विकसित मूल वेबसाइटों की बराबरी पर नहीं हैं । लिहाजा घूमफिर कर अंगरेजी की ही शरण में जाना पड़ता है । देश के किसी विश्वविद्यालय की वेबसाइट में हिंदी को स्थान मिला भी होगा इसमें मुझे शंका है ।
इस प्रकार के अनेकों उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि इस देश के प्रबंधकों को हिंदी में कोई रुचि नहीं है । ऐसे में हिंदी के राजभाषा होने का अर्थ ही क्या रह जाता है ? और तब किस उद्येश्य से हिंदी दिवस मनाया जाये ? अंगरेजी का वर्चस्व आज तो है ही, कल भी बना रहेगा, अंतर पड़ना नहीं है, तब यह रस्मअदायगी ही क्यों ? – योगेन्द्र


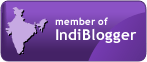
सितम्बर 14, 2009 at 1:00 अपराह्न
आपका कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि .. अपना देश विचित्र,अजूबा, विरोधाभासों और विसंगतियों से परिपूर्ण है .. बहुत सही प्वाइंट्स हैं आपके .. पर सिर्फ यही एक क्षेत्र ही ऐसा नहीं .. जहां सरकारी कर्मचारियों की भूमिका नगण्य है .. कमोबेश हर क्षेत्र का यही हाल है .. सरकार के पैसों का दुरूपयोग हो रहा है .. ब्लाग जगत में आज हिन्दी के प्रति सबो की जागरूकता को देखकर अच्छा लग रहा है .. हिन्दी दिवस की बधाई और शुभकामनाएं !!
सितम्बर 14, 2009 at 2:38 अपराह्न
(आगे उल्लिखित शब्द उस टिप्पणी के हैं जिसका संदर्भगत चिट्ठे से सीधा संबंध नहीं है | फिर भी यह पाठकों के लिए उपयोगी हो सकता है | अतः इसे मिटाया (डिलीट) नहीं गया है |- योगेन्द्र जोशी)
Just install Add-Hindi widget button on your blog. Then u can easily submit your pages to all top Hindi Social bookmarking and networking sites.
Hindi bookmarking and social networking sites gives more visitors and great traffic to your blog.
Click here for Install Add-Hindi widget
सितम्बर 13, 2015 at 8:19 पूर्वाह्न
hindi bhasa ko kab angikrit kiya gaya
जुलाई 7, 2016 at 8:31 पूर्वाह्न
हिन्दी को राजभाषा के रूप में संविधान सभा द्वारा १४ सितंबर १९४९ को स्वीकारा गया।