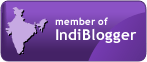श्री शशिशेखर जी,
मैंने आपका लेख “हत्भागिनी नहीं हमारी हिंदी” (हिन्दुस्तान, सितंबर 8) पढ़ा । उसी के संदर्भ में अपनी टिप्पणी प्रेषित कर रहा हूं । (अपने ब्लॉग https://hinditathaakuchhaur.wordpress.com में भी मैं इसे शामिल कर रहा हूं ।)
प्रथमतः मैं निवेदन करता हूं कि ‘हत्भागिनी’ न होकर ‘हतभागिनी’ होना चाहिए था । शब्द हत (मारा गया) है न कि हत् । शीर्षक में यह त्रुटि खलती है; अन्यथा चल सकता था । इस धृष्टता के लिए क्षमा करें ।
देश-विदेश में हिंदी, पर कितनी?
लेख में आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हिंदी देश-विदेश में विस्तार पा रही है और अधिकाधिक लोग इसे प्रयोग में ले रहे हैं । आपने जिन अनुभवों की बात की है वे कमोवेश सभी को होते हैं, खास तौर पर इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका में । सीधा-सा तथ्य यह है कि जहां कहीं भी पर्याप्त संख्या में हिंदीभाषी/उर्दूभाषी लोग रह रहे हैं, या बस चुके हैं, वहां उनके बीच हिंदी का प्रचलन देखने को मिल जाता है । जब विदेश में अपने देश अथवा भाषाई-सांस्कृतिक दृष्टि से निकटता रखने वाले अन्य देशों के निवासी पहुंचते हैं, तब उनमें परस्पर अपनापन का भाव जगता है यह स्वयं मेरा अनुभव रहा है ।
जब मैं 1983-85 में साउथहैम्पटन (इंग्लैंड) में था तब भारतीयों एवं पाकिस्तानियों से मेरी हिंदी में ही बात होती थी । लंडन के पास साउथहॉल का नजारा कुछ ऐसा हुआ करता था कि वहां पहुंचने पर ‘हम भारत में हैं’ ऐसा लगता था । साउथहैम्पटन में गुजराती दुकानदारों से मैं भारतीय भोजन सामग्री खरीदते समय अक्सर हिंदी में बात करता था । आरंभ में मैं एक पाकिस्तानी खान साहब के मकान में रहा, उनसे हिंदी में बात होती थी । बाद में किसी पंजाबी सज्जन के मकान में रहा जिसके पड़ोस में पंजाबी परिवार रहता था । उस परिवार की हिंदी-पंजाबी बोलने वाली महिला से मेरी पत्नी के अच्छे ताल्लुकात हो चले थे । मुझे एक पाकिस्तानी महोदय की याद है जिन्होंने कहा था, “आप लोग हिंदी बोलने की बात करते हैं, क्या यही हिंदी है, उर्दू जैसी ?”
उन दिनों भारत सरकार हवाई अड्डे पर मात्र 12-13 पौंड की रकम देती थी । मैं जब साउथहैम्पटन पहुंचा तो पता चला कि उस दिन सार्वजनिक छुट्टी है । उसके तथा विदेश यात्रा का पूर्ववर्ती अनुभव न होने के कारण तब मुझे काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी । उस दिन एक बांग्लादेशी मूल के रेस्तरांवाले ने मुझे मुफ्त में भोजन कराया था ।
अमेरिका (सिलिकॉन वैली) में भी मेरे अनुभव कुछ मिलते-जुलते रहे । मेरे बेटे के हिंदुस्तानी साथियों के बीच हिंदी-अंगरेजी में वार्तालाप सामान्य बात होती थी । वहां बसे उसके एक मित्र के 5-7 साल के बच्चों को हिंदी में बोलते देख मुझे आश्चर्य हुआ । पता चला कि वे गरमियों में भारत आकर दादा-दादी के पास ठहरते हैं और हिंदी सीखते हैं ।
कहने का मतलब है कि दुनिया के जिन हिस्सों में पर्याप्त संख्या में हिंदीभाषी मूल के लोग हैं वहां वे प्रायः आपका स्वागत करेंगे और हिंदी बोलते हुए भी दिख जाएंगे ।
मुझे पता चला कि कैलिफोर्निया में कुछ प्राथमिक विद्यालयों में चीनी भाषा भी पढ़ाई जाती है । संप्रति अमेरिका में यह सर्वाधिक सीखी जा रही भाषा है । वहां कई चीनी/कोरियाई मूल के लोगों की दुकानों पर नामपट्ट तक संबंधित लिपि में देखने को मिलते हैं । वहां के एक ‘कंडक्टेड टूअर’ का अनुभव मुझे याद है जिसका गाइड ताइवान मूल का युवक था, जिसने अपनी कमजोर अंगरेजी एवं मजबूत चीनी भाषा में पर्यटक स्थलों का परिचय कराया था । साथ में उपलब्ध पाठ्यसामग्री चीनी एवं अंगरेजी, दोनों में, थी । इस माने में हिंदी एकदम पीछे है ।
आपके-मेरे सरीखे अनुभव संतोष करने के लिए काफी नहीं हैं ऐसा मेरा मानना है । आपने इन दो बातों पर खास कुछ नहीं कहा:
(1) पहला, जो हिंदी अब पढ़ेलिखे लोगों के बीच जड़ें जमा रही है वह दरअसल हिंदी-अंगरेजी का मिश्रण है, और
(2) दूसरा, लिखित रूप में हिंदी की प्रगति निराशाप्रद ही है ।
हिंदी-अंगरेजी मिश्रभाषा
(1) जिस प्रकार यह देश ‘इंडिया’ तथा ‘भारत’ में बंटा है वैसे ही हिंदी (और कदाचित अन्य भारतीय भाषाएं) भी दो श्रेणियों में बंटी है । पहली को मैं व्यक्तिगत तौर पर मैट्रोहिंदी कहता हूं । इसे आप ‘महानगरीय हिंदी’, ‘एंग्लिसाइज्ड हिंदी’, ‘एंग्लोहिंदी’, अथवा ‘हिंदी-इंग्लिश मिश्रभाषा’ या कुछ और नाम दे सकते हैं । यह उन लोगों की भाषा है जो इस देश को ‘भारत’ नहीं कहते बल्कि ‘इंडिया’ कहते हैं । आप बताइए कितने पढ़ेलिखे लोगों के मुख से भारत शब्द निकलता है ? यह उस देश के हाल हैं जहां लोग मुंबई, चेन्नई, पुणे, पश्चिमबंग, ओडिशा, आदि नामों के लिए अभियान चलाते हैं, लेकिन देश को इंडिया कहना पसंद करते हैं । यह उन शिक्षित लोगों की भाषा है जो अंगरेजी के इस कदर आादी हो चुके हैं कि उन्हें समुचित हिंदी शब्द सूझते ही नहीं अथवा उन्हें याद नहीं आते हैं । आज स्थिति यह है कि ‘एंड’, ‘बट’, ‘ऑलरेडी’ आदि शब्द जुबान पर तैरते रहते हैं । कुछ लोग शारीरिक अंगों, ‘किड्नी’, ‘लिवर’, ‘मशल’ आदि और ‘ग्रे’, ‘मरून’ आदि जैसे रंगों की हिंदी बताने में भी असमर्थ पाये जाएंगे । हिंदी की गिनतियां अब जुबान पर कम ही आती हैं । कितने उदाहरण दें ? इस भाषा में अंगरेजी शब्द ही नहीं, वाक्यांश या पूरे वाक्य भी शामिल रहते हैं । पर्याप्त अंगरेजी न जानने वाले की समझ से परे ‘कम्यूनिके’, ‘कॉर्डन-आफ’, ‘सेफ्टी मेजर्स’ जैसे शब्दों का प्रयोग आम हो चला है । यह सब हो रहा है इस कुतर्क के साथ कि इससे हमारी हिंदी समृद्ध होती है । लेकिन अंगरेजी की शुद्धता के लिए वे पूर्णतः सचेत रहते हैं । उसको भी समृद्ध क्यों नहीं बनाते ?
दूसरी तरफ हमारी ‘देसी’ हिंदी है जो ग्रामीणों, अशिक्षितों/अल्पशिक्षितों, श्रमिकों आदि के द्वारा बोली जाती है, जिनका अंगरेजी ज्ञान अपर्यााप्त रहता है । उस हिंदी की बात होती ही कहां है ?
यह ठीक है कि अभी उक्त मिश्रभाषा का प्रयोग साहित्यिक कृतियों में नहीं हो रहा है, लेकिन टीवी चैनलों पर तो यही अब जगह पा रही है । विज्ञापनों की भाषा भी यही बन रही है । दिलचस्प तो यह है कि इस भाषा की लिपि भी देवनागरी एवं रोमन का मिश्रण देखने को मिल रहा है । इंटरनेट पर रोमन में लिपिबद्ध हिंदी खुलकर इस्तेमाल हो रही है, जब कि फोनेटिक की-बोर्ड के साथ यूनिकोड में टाइप करना कठिन नहीं होता ।
आशाप्रद नहीं लिखित हिंदी की स्थिति
(2) निःसंदेह हिंदी – अंगरेजी मिश्रित ही सही – एक बोली के रूप में विस्तार पा रही है । लेकिन लिखित तौर पर इसका इस्तेमान कितना हो रहा है ? एक ओर सरकारें इसे संघ की राजभाषा कहती हैं अैर दूसरी ओर वही इससे परहेज रखती हैं । ऐसे में अधिक उम्मीद कैसे की जा सकती है ? लोग बातें तो हिंदी में करते हैं, लेकिन लिखित में कुछ बताना हो तो अंगरेजी पर उतर आते हैं । डॉक्टर मरीज से हिंदी में करता है किंतु नुसखा अंगरेजी में ही लिखता है, इस बात की परवाह किए बिना कि मरीज उसे समझ पाएगा या नहीं । लिफाफे पर पता, रेलवे आरक्षण फॉर्म, बैंक लेनदेन का फॉर्म, इत्यादि वे अंगरेजी में ही भरते हैं, अगर वे अल्पशिक्षित न हों तो । कितनी सरकारी संस्थाएं आप गिना सकते हैं जिनकी वेबसाइटें हिंदी में हैं; अगर कहीं हैं तो अधकचरे । इंटरनेट पर कितने फार्म हैं जिन्हें देवनागरी में भरने का विकल्प उपलब्ध हो ? रेलवे आरक्षण टिकट हों या बिजली/टेलीफोन बिल उनकी प्रविष्टियां अंगरेजी में ही मिलेंगी ! जिस देश की सर्वोच्च अदालत ‘नो हिंदी’ कहे, यूपीएससी जैसी संस्था ‘अंगरेजी कंपल्सरी’ कहे, वहां हिंदी का भविष्य कैसा होगा सोचा जा सकता है ।
देश की व्यावसायिक संस्थाओं ने तो जैसे कसम खा रखी है कि वे हिंदी हरगिज नहीं चलने देंगे । बाजार में उपलब्ध उपभोक्ता सामग्री के बारे में कितनी संस्थाएं हिंदी-देवनागरी में जानकारी देती हैं ? बिस्किट पैकेट हो या टूथपेस्ट या अन्य उत्पाद उन पर हिंदी दिख जाए तो अहोभाग्य । कंप्यूटर संबंधी उपस्करों के साथ उपलब्ध जानकारी वियतनामी, थाई, हिब्रू, आदि में मिल जाएगी, लेकिन भारतीय भाषाओं में नहीं । हिंदीभाषी क्षेत्रों के दिल्ली या अन्य बड़े शहरों में घूम जाइए, आपको हिंदी में शायद ही कहीं नामपट्ट दिखें ।
इस बात से आप अगर संतुष्ट हों कि अब अधिक लोग हिंदी बोल रहे हैं, भले ही उसे विकृत कर रहे हों, और उसे न लिखने की कसम खाए हों तो खुशकिस्मत हैं । लेकिन मुझे इसमें संतोष की गुंजाइश नहीं दिखती ।
भवदीय,
योगेन्द्र जोशी
राष्ट्र संघ आधिकारिक भाषा दिवस
इसी वर्ष (2010) संयुक्त राष्ट्र संघ (UNO) ने अपनी 6 आधिकारिक भाषाओं (official languages) के नाम पर ‘दिवस’ घोषित किये हैं । (देखें http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=34469&Cr=multilingual&Cr1=) ये दिवस इस प्रकार हैं:
1. अरबी भाषा दिवस Arabic Language Day (दिसम्बर 18 December) | सन्1973 की इसी तिथि पर अरबी भाषा को संयुक्त राष्ट्र संघ की छःठी आधिकारिक भाषा (Official Language) की मान्यता दी गयी थी ।
2. चीनी भाषा दिवस Chinese Language Day (अप्रैल 20 April) । चीनी चांद्रमास के अनुसार यह दिन चीन में ‘अन्न दिवस’ (Day of Grain) के तौर पर मनाया जाता है ।
3. अंग्रेजी भाषा दिवस English Language Day (अप्रैल 23 April) | यह दिन प्रसिद्ध अंग्रेजी नाट्यकार विलियम शेक्सपियर (William Shakespeare) के जन्मदिन के तौर जाना जाता है ।
4. फ़ांसीसी भाषा दिवस French Language Day (मार्च 20 March) | संयोग से यह दिन फ़्रांसीसी-प्रेमियों और फ़ांसीसी भाषा का मानवीय मूल्यों के संवर्धन में योगदान के नाम पर बने उनके संगठन ‘ला फ़्रांकोफ़ोनी’ (La Francophonie) का स्थापना दिवस है ।
5. रूसी भाषा दिवस Russian Language Day (जून 6 June) । यह दिन अलेक्ज़ांडर पुश्किन (Aleksander Pushkin), जिन्हें रूसी साहित्य के जनक के तौर पर देखा जाता है, का जन्मदिन है ।
6. स्पेनी भाषा दिवस Spanish Language Day (अक्टूबर 12 October) । यह स्पेन का राष्ट्रीय दिवस तथा स्पेनी भाषा-संस्कृति मानने वाली अन्यत्र वसी बिरादरी (Hispaniards) के दिवस के तौर पर जाना जाता है ।
संघ के महासचिव ने पहली बार मनाये गये ‘अंग्रेजी दिवस’ – 23 मार्च – के अवसर पर शेक्सपियर के शब्दों, `a feast of languages’ (भाषाओं का भोज, विविध भाषाओं की दावत), को उद्धरित करते हुए इन दिवसों की अहमियत को रेखांकित किया था । बहुभाषाभाषी इस विश्व में सभी भाषाओं को सम्मान मिले, और संघ के कार्यों में उक्त सभी भाषाएं समान रूप से प्रयुक्त हों यह संघ का प्रयास रहेगा ऐसी भावना इन दिवसों से जुड़ी है ।
अंग्रेजी के संदर्भ में मुझे एक वेबसाइट पर यह भी पढ़ने को मिला हैः “13 अक्टूबर 1362 में इंग्लैंड के ‘चांसलर’ ने पार्लियामेंट का उद्घाटन पहली बार अंग्रेजी भाषा में किया । सभा के उसी सत्र में विधि-नियमों और विधिक कार्यों के लिए सभा-सदस्यों को अंग्रेजी के प्रयोग की अनुमति दी गई । इस दिन को ‘अंग्रेजी भाषा दिवस’ (English Language Day) माना जाता है ।” लेकिन राष्ट्र संघ का घोषित अंग्रेजी दिवस इससे भिन्न है । (देखें http://www.englishproject.org/index.php?option=com_content&view=article&id=592&Itemid=472)
दिवसों की भरमार
पिछले कुछ दशकों से दिवसों का चलन बढ़ गया है । मानव समाज की हर समस्या की ओर ध्यानाकर्षण के लिए नये-नये दिवस घोषित किये जा रहे हैं । उपर्युक्त दिवस उसी फैशन की नई बानगी हैं । अब देखिए इसी माह (सितंबर) के उन दिवसों की सूची जिनकी जानकारी मुझे मिल सकी है:
(अंतर० = अंतरराष्ट्रीय; Intl. = International)
8 Intl. Literacy Day अंतर० साक्षरता दिवस
11 World First Aid Day विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस
14 Intl. Cross-Cultural Day अंतर० मिश्रसंस्कृति दिवस
15 Intl. Day of Democracy अंतर० लोकतंत्रता दिवस
3rd Tuesday Intl. Day of Peace अंतर० शांति दिवस
16 Intl. Day for Ozone Preservation अंतर० ओजोन संरक्षण दिवस
20 Intl. Car Free Day अंतर० कारमुक्त दिवस
21 World Alzheimer’s Day अंतर० अल्जाइमर दिवस
21 Intl. Day of Peace अंतर० शान्ति दिवस
23 World Deaf Day विश्व बधिर दिवस
27 World Tourism Day विश्व पर्यटन दिवस
28 World Heart Day विश्व हृदय दिवस
28 World Rabies Day विश्व रेबीज़ दिवस
अस्तु, ये हैं विश्व दिवस । राष्ट्रीय स्तर के दिवस, जो भी हों, अतिरिक्त हैं । इसी माह 5 तारीख ‘शिक्षक दिवस’ मनाया जा चुका है । 14 तारीख हिंदी दिवस है ही । इसी वर्ष कुछ पर्यावरणविदों और उत्साही नागरिकों ने ‘हिमालय दिवस’ भी मनाया है, 9 तारीख, हिमालय क्षेत्र के बिगड़ते पर्यावरण के प्रति सरकार एवं आम जनों का ध्यान आकर्षित करने के उद्येश्य से । अब भविष्य में यह भी मनाया जाएगा । (http://www.thaindian.com/newsportal/enviornment/environmentalists-observe-himalaya-day_100425964.html)
दिवसों की अहमियत
हमारे देश में त्यौहारों-पर्वों के रूप में अनगिनत ‘दिवस’ मनाने की परंपरा चली आ रही है । इनका उद्येश्य समझ में आता हैः जीवन के प्रतिदिन के कार्यव्यापार से हटकर मनोरंजन एवं सांस्कृतिक-सामाजिक संपर्कों का प्रयोजन इनमें निहित रहता है । ईद-दीवाली, बीहू-बैशाखी एवं अन्य धार्मिक पर्व इस श्रेणी में आते हैं । अपने यहां दिवंगत महापुरुषों के जन्मदिनों की भी भरमार है, जैसे बुद्ध, गांधी, नेहरु, अंबेडकर जयंतियां । बीते वर्षों में गुजरते समय के साथ नये-नये दिवस इस श्रेणी में जुड़ते चले गये हैं । कुछ दिवसों पर कार्यालयिक छुट्टी होती है, तो कुछ पर विविध आयोजन । मदर्स डे, फ्रेंड्ज डे, वैलंटाइन डे, न्यू इयर्स डे जैसे दिन भी हाल के वर्षों में दिवसों की सूची में जुड़ चुके हैं । इन पर अवकाश भले ही न हो, लोगों का जोश देखने योग्य होता है । इन सब का महत्त्व व्यक्तियों अथवा समुदाय-विशेषों के लिए ही अधिक है ।
हाल के वर्षों में सामाजिक सरोकारों तथा पर्यावरण से संबद्ध दिवस सूची में और जुड़ चुके हैं, जो अधिकतर वैश्विक स्तर के हैं । ये ही वे दिवस हैं जो जाति, धर्म, क्षेत्र से परे राष्ट्रीय अथवा अंताराष्ट्रीय अहमियत रखते हैं । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि से जुड़े दिवस अपना अलग महत्त्व रखते हैं, जैसे अंताराष्ट्रीय ‘पृथ्वी दिवस’ (22 अप्रैल), ‘पर्यावरण दिवस’ (5 जून), ‘जनसंख्या दिवस’ (11 जुलाई), ‘भ्रष्टाचार निवारण दिवस’ (9 दिसंबर), आदि । मुझे शंका है कि इनमें से कइयों का अखबारों में जिक्र तक नहीं होता है । ये वे दिवस हैं, जब रस्मअदायगी से आगे बढ़कर कुछ कर गुजरने का संकल्प नागरिकों को लेना होता है । ये दिन हैं जब मुद्दों पर संजीदा हुआ जाना चाहिए । अगर ऐसा नहीं होता है तो फिजूल है उस दिवस का मनाया जाना । हिंदी दिवस ऐसा ही एक दिवस है ।
हिंदी दिवसः खो चुकी अहमियत
“… राजभाषा समिति की बैठक में हिंदी की जगह अंग्रेजी की उपस्थिति पर न केवल हंगामा हुआ, बल्कि भाजपा सदस्यों ने तो अंग्रेजी दस्तावेज को फाड़ कर और बैठक का बहिष्कार कर विरोध भी दर्ज कराया। गृहमंत्री तो बैठक में आए ही नहीं। … बैठक उस समय हंगामे में डूब गई जब कुछ दस्तावेज हिंदी के बजाय अंग्रेजी में पेश किए गए। … सदस्यों ने याद दिलाया कि राजभाषा अधिनियिम की धारा 3 [3] के तहत हिंदी में दस्तावेज होना जरूरी है, अधिकारी ने जवाब दिया कि यह उनके मंत्रालय पर लागू नहीं होता। … समिति के अध्यक्ष होने के बावजूद गृहमंत्री पी. चिदंबरम बैठक में आए ही नहीं। पिछले साल बैठक में वह आए थे तो उन्होंने भाषण अंग्रेजी में दिया था।” (स्रोत: http://in.jagran.yahoo.com/news/national/politics/5_2_6709123.html)
समाचार यहां भी पढ़ सकते हैं: http://epaper.amarujala.com/svww_index.php
उक्त समाचार साफ दिखलाता है कि बतौर राजभाषा के हिंदी के प्रति देश की नौकरशाही का क्या रवैया है । अंग्रेजी के वर्चस्व को कैसे बनाये रखा जाए और उसके लिए क्या-क्या बहाने रचे जाएं इसे आप उनसे सीख सकते हैं । निर्लज्ज अधिकारियों का ढीठपन देखिए, कहते हैं: “राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) उनके मंत्रालय पर लागू नहीं होती है, गोया कि उनका मंत्रालय अपवाद है और संविधान ने कुछ मंत्रालयों को राजभाषा न इस्तेमाल करने की छूट दे रखी है ।” अवश्य ही सुप्रीम कोर्ट (उच्चतम न्यायालय?) एक हास्यास्पद अपवाद है, जिसके लिए केवल अंग्रेजी ही मान्य है! दुर्भाग्य से देश का प्रबंधन जनसंख्या के शीर्ष पर बैठी 10% से कम जिस अभिजात वर्ग के हाथ में है उसे यह हरगिज बर्दास्त नहीं है कि भारतीय भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी का वर्चस्व घटे । इस वर्चस्व को बनाये रखने के लिए वे हर मुमकिन कोशिश करने को तैयार हैं । अगर वे ऐसा न करें तो अंग्रेजी के कारण जिस लाभ की स्थिति में वे हैं वह नहीं रहेगी । कोई भी चालाक व्यक्ति और व्यक्ति-समूह अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता ।
मुझ जैसे लोगों के लिए यह एक पीड़ादायक तथ्य है कि अपना देश हिंदुस्तान एक बुरी तरह विभाजित समाज है । यहां एक नहीं कई विभाजक कारक हैं: जाति, धर्म, क्षेत्र, आर्थिक संपन्नता तो हैं ही, उन सब के ऊपर है अंग्रेजी – अंग्रेजी जिसने एक ही राष्ट्र को ‘इंडिया और भारत’ में बांट रखा है । पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इंडिया के हाथ में है, जो अंग्रेजी के वर्चस्व का घोर पक्षधर है ।
निस्संदेह हिंदी आम बोलचाल की भाषा है; दिल्ली के सचिवालय के गलियारों में भी यही बोली जाती है । आगे भी बोली जाएगी, भले ही ऐसा उसके वर्णसंकर अवतार ‘हिंग्लिश’ के रूप में हो । बोलचाल में वह विस्तार भी पा रही है, और देश के कोने-कोने में पहुंच भी रही है । किंतु उसके आगे बढ़कर वह दस्तावेजी भाषा नहीं बन सकती है । इसीलिए वह असल राजभाषा नहीं बन सकती, भले ही राजभाषा का ‘खिताब’ इसे मिला हो ! … कभी भी नहीं ।
तब फिर हिंदी दिवस की अहमियत क्या है? किसे याद दिलाने के लिए है यह दिवस ?
अंत में
राजभाषा संसदीय समिति का अध्यक्ष केंद्र सरकार के गृहमंत्री हुआ करते हैं – पदेन । अपने गृहमंत्री हिंदी नहीं जानते हैं – शायद बिल्कुल नहीं जानते हैं, और न ही जानने की इच्छा रखते हैं । यों तो सरकार चलाने वाले शीर्ष स्तर के राजनेता और प्रशासनिक अधिकारियों को हिंदी में कोई दिलचस्पी नहीं रहती है, भले ही वे हिंदीभाषी क्षेत्र के ही क्यों न हों, भले ही उनकी घोषित मातृभाषा हिंदी ही क्यों न हो । उन्हें हिंदी से अघोषित परहेज दृ सख्त लहजे में कहूं तो विरोध – रहता ही रहता है । फिर भी हिंदी दिवस जैसे मौके पर वे हिंदी में बोलने की रस्मअदायगी करते ही हैं । किंतु तमिलनाडु के राजनेता (आम आदमी उतना नहीं!) हिंदी से कतराते जरूर हैं । परहेज रखना शायद उनकी राजनीतिक विवशता है । दरअसल तथाकथित ‘द्रविड़’ पार्टियों के जन्म एवं उत्थान का आधार ही हिंदी विरोध रहा है । उन्हें यह विरोध बरकरार रखना है । इस हालत में कांग्रेस जैसी पार्टियां यह साहस नहीं दिखा सकती हैं कि वे हिंदी के पक्ष में नजर आवें । हिंदी के प्रति असली या नकली विरोध उन्हें भी दिखाना ही होता है । इस कारण से हिंदी का ‘मूक’ विरोध करना अपने गृहमंत्री की मजबूरी है । मैंने अभी तक कोई ‘तमिल’ राजनेता नहीं देखा है, जिसने कभी भी दो शब्द हिंदी में बोले हों । – योगेन्द्र जोशी