कितनी सार्थक है हिंदी की ‘राजभाषा’ उपाधि?
जून 17, 2009
पिछले कुछ समय से मैं एक प्रश्न का ‘संतोषप्रद’ उत्तर (महज उत्तर नही, संतोषप्रद उत्तर!) पाने की चेष्टा कर रहा हूं । हमारे संविधान निर्माताओं ने हिंदी को देश की राजभाषा घोषित किया । क्या सोचकर किया इसे तो ठीक-ठीक वही समझते रहे होंगे । आज हम इसलिए-उसलिए कहते हुए तब के सोचे गये कारणों की व्याख्या अवश्य कर सकते हैं । परंतु क्या कारणों को समझ लेना ही पर्याप्त है ? हममें से अधिकांश जन यही कहेंगे कि हिंदी को राजभाषा तो होना ही चाहिए था, और इसलिए वह राजभाषा मानी भी गयी । परंतु क्या वह वास्तव में राजभाषा बन सकी है या राजभाषा उसके लिए एक अर्थहीन उपाधि बनकर रह गयी है ? क्या वह बतौर राजभाषा प्रयुक्त हो रही है ? मैं स्वयं से पूछता हूं कि क्या संविधान द्वारा हिंदी को ‘दी गई’ राजभाषा की उपाधि सार्थक है ।
मुझे उक्त प्रश्न का उत्तर नकारात्मक मिलता है । राजभाषा होने के क्या मतलब हैं, और हकीकत में जो होना चाहिए वह किस हद तक हो रहा है, इन बातों की समीक्षा की जानी चाहिए । आज हिंदी को राजभाषा घोषित हुए साठ वर्ष होने को हैं । आप कहेंगे साठ वर्ष बहुत नहीं होते हैं किसी राष्ट्र के जीवन में । लेकिन यह भी सच है कि इतना लंबा अंतराल कुछ कम भी नहीं होता है । बात यूं समझिएः पदयात्रा पर निकला व्यक्ति दिन भर में औसतन 20-25 किलोमीटर चल सकता है । 20-25 नहीं तो 15-20 कि.मी. ही सही, या थोड़ा और कम की सोचें तो 12-15 कि.मी. तो चलना ही चाहिए । हम उससे 9 दिन में हजार-पांचसौ कि.मी. की पदयात्रा की अपेक्षा नहीं कर सकते । लेकिन सौ-डेड़सौ की उम्मीद करना तो गैरवाजिब नहीं होगा न ? यदि ‘नौ दिन चले अढाई कोस’ वाली बात घटित हो रही हो, तो क्या संतोष किया जा सकता है ? अपनी राजभाषा का हाल कुछ ऐसा ही है । सो कैसे इसे स्पष्ट करने का विचार है मेरा इस और आगामी पोस्टों में ।
अपने अध्ययन तथा चिंतन (मेरा विश्वास है कि मैं कुतर्क नहीं कर रहा हूं) की बात करने से पहले में संविधान द्वारा राजभाषा घोषणा संबंधी कुछ शब्दों की चर्चा करना चाहता हूं । देश के संविधान में हिंदी को ‘संघ की राजभाषा’ घोषित किया गया है । संविधान सभा की बैठक सन् 1949 में 12 से 14 सितंबर तक चली थी, जिसमें संविधान को मौलिक तथा अंतिम रूप दे दिया गया और कालांतर में वह 26 जनवरी, 1950, से प्रभावी भी हो गया । उस बैठक के अंतिम दिन (14 सितंबर) काफी जद्दोजेहद के बाद संघ की भाषा के रूप में हिंदी को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया । हिंदी को उस दिन मिली ‘राजभाषा’ की उपाधि और तत्पश्चात् अगले वर्ष (1950) की उसी तारीख से बतौर केंद्र सरकार के राजकाज की भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के आरंभ की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर का दिन ‘हिंदी दिवस’ के रूप में मनाया भी जाता है । दिवस मनाने का यह सिलसिला तब से चला आ रहा है, कुछ हद तक साल दर साल घटते उत्साह के साथ और विशुद्ध औपचारिकता की भावना से !
तब संगठित संविधान सभा के अध्यक्ष डा. राजेन्द्र प्रसाद थे जिन्हें नये संविधान के अनुरूप देश का प्रथम राष्ट्रपति चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ । उस बैठक में भाव-विभोर होकर उन्होंने कहा था:
“आज पहली ही बार ऐसा संविधान बना है जब कि हमने अपने संविधान में एक भाषा रखी है, जो संघ के प्रशासन की भाषा होगी । इस अपूर्व अध्याय का देश के निर्माण पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । … अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया । इससे अवश्य ही हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएं एक हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं । … हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है और मुझे हर्ष है, मुझे प्रसन्नता है और मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी ।”
ज्ञातव्य है कि संविधान सभा की भाषा विषयक बहस अधिकांशतः अंग्रेजी में ही संपन्न हुई और तत्संबंधित दस्तावेज अंग्रेजी में ही तैयार हुआ, जो 278 पृष्ठों में छपा है । सभा की बैठक में अध्यक्ष के उद्गार भी, मेरे अनुमान से, अंग्रेजी में ही अभिव्यक्त थे । ऊपर केवल कुछ चुने हुए वाक्य उल्लिखित हैं । अंग्रेजी मूल का मेरा स्वयं-संपादित अनुवाद स्वीकार्य होना चाहिए ऐसी आशा की जाती है ।
संविधान सभा के अध्यक्ष का संघ की भाषा के प्रति आशावाद कितना सार्थक सिद्ध हुआ इसका आकलन करना कठिन नहीं है । तब कदाचित् सभा के सदस्यों को इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि भविष्य में वह सब नहीं होने जा रहा है, जिसकी सुखद कल्पना वे उस काल में कर रहे थे । अध्यक्ष द्वारा कहे गये कुछएक वाक्यों/वाक्यांशों पर गौर करें:
§ “अंग्रेजी के स्थान पर हमने एक भारतीय भाषा को अपनाया ।” ठीक किया ? शायद नहीं । माफ करें, वैयक्तिक स्तर पर यह मेरे चाहने न चाहने का सवाल नहीं है । जो हकीकत सामने है वह यही कहती है कि यह सोच गलत साबित हो रही है । मुझे यह कहते खुशी नहीं है; पर सच तो सच है, आप चाहें या न चाहें ।
§ “इससे अवश्य ही हमारे संबंध घनिष्ठतर होंगे, विशेषतः इसलिए कि हमारी परंपराएं एक हैं, हमारी संस्कृति एक ही है और हमारी सभ्यता में सब बातें एक ही हैं ।” तब क्यों अंगरेजी के पक्षधर यह दलील देते हैं कि पूरे देश में यदि कोई भाषा प्रचलन में है तो वह अंगरेजी ही है ? क्यों कहते हैं कि देश भर का राजकाज अंगरेजी के बिना नामुमकिन है, इत्यादि ?
§ “हमने यथासंभव बुद्धिमानी का कार्य किया है ।” जिस भाषा की उपस्थिति देश के शासन-प्रशासन में अभी तक न के बराबर चल रहा है उसे राजभाषा का दर्जा देना कैसे बुद्धिमत्ता हो सकती है । हमारे नीतिनिर्धारकों और प्रशासकों का बल तमाम दलीलें देता आया है और हिंदी में धेले भर का काम तक करने को तैयार नहीं उसके बाबत बुद्धिमानी की बात करना गले के नीचे नहीं उतरती है ।
§ “मुझे आशा है कि भावी संतति इसके लिए हमारी सराहना करेगी ।” आज की जो पीढ़ी भारतीय भाषाओं को दोयम दरजे का मानकर चल रही हैं और जो कहती फिर रही है कि उनकी वैयक्तिक प्रगति और देश का समग्र विकास अंगरेजी के बिना संभव ही नहीं, वह पीढ़ी क्या वास्तव में संविधान निर्माताओं के निर्णय की सराहना कर रही है । जो युवा पीढ़ी अपना सब कार्य अंगरेजी में निबटाने को आतुर हो, वह क्या हिंदी को राजभाषा के अनुरूप सम्मान दे रही है, देना चाहती है ? मुंह से भले ही नकारात्मक कुछ न कहा जा रहा हो, किंतु जो घट रहा है उससे स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं क्या ?
इनकी और इनके अतिरिक्त अन्य बातों की चर्चा मुझे करनी है । चर्चा अगली पोस्टों में जारी रहेगी । – योगेन्द्र
Filed in अंग्रेजी, भारत, राजभाषा, हिन्दी, English, Hindi, India
टैग्स: भारतीय संविधान, संविधान सभा, हिंदी दिवस, constitutional bench, Hindi Divas, Indian Constitution, Official language, Tags: राजभाषा


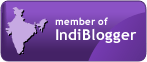
जून 18, 2009 at 9:22 पूर्वाह्न
जी हॉ, हिंदी का राजबाषा नाम सार्थक है क्योंकि राजभाषा की शब्दावली आदि केवल राजकीय कामकाज में उपयोग में ला जाते हैं। प्रत्येक राष्ट्र में राजभाषा और आम बोलचाल की भाषा में फर्क होता है जो सर्वविदित है।
राजभाषा को जो हकीकत में होना चाहिए यदि वह नहीं है तो इसका दायित्व राजभाषा के उपयोगकर्ताओं का है अर्तात कार्यालय कर्मियों का जिसमें राजभाषा अधिकारी भी सम्मिलित हैं।
हिंदी दिवस मनाया जाना राजभाषा कार्यान्वयन की वह प्रकिर्या है जिससे राजभाषा के प्रेरणा और प्रोत्साहन को एकीकृत किया जाता है। राजभाषा का यह एक उत्सव है। यदि कोई उत्सव उत्साहपूर्वक न मनाए तो भला उसमें उत्सव का क्या दोष।
आपके मुद्दों में एक जोश है किंतु तमाम कमियों के बावजूद भी राजभाषा प्रगति कर रही है। राजभाषा विषयक प्रस्तुति अच्ची लगी, बस नाराज़गी का पुट कुछ अधिक लगा।
जून 26, 2019 at 2:19 अपराह्न
संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुतासंपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है. यह गणराज्य भारतीय संविधान (Bhartiya Samvidhan) द्वारा शासित है. भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ।
सितम्बर 15, 2019 at 3:33 अपराह्न
संविधन सभा ने क्या पारित किया यह तब अहम होता जब देश के राजनेता उसको महत्व देते। संविधान में बहुत-सी बातें है जो होनी चाहिए लेकिन आज के नेताओं का उससे विरोध है। कल अमित शाह ने हिन्दी के पक्ष में कुछ बोल क्या दिया सब तरफ से विरोध के स्वर उठने लगे हैं। संविधान के दिशानिर्देशक सिद्धान्तों (Directive Principles) के अनुसार सरकारों दायित्व होगा कि वे समान नागरिक संहिता (Common Civil Code) स्थापित करने की दिशा में बढ़ें। किंतु आज खुलकर कहा जाता है कि यह किसी भी हालत में स्वीकार्य नहीं। देश को सेक्युलर कहा गया है। सेक्युलर क्या होता इस शब्द के इतिहास में जाना पड़ेगा। संक्षेप में यह कहता है कि शासकीय व्यवस्था किसी भी धर्म पर आधारित नहीं होगा। क्या भरत में ऐसा है? कल यदि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनने की बारी आयेगी तो कहा जाएगा कि देश सांप्रदायिकता की ओर बढ़ रहा है। इस लोकतंत्र में यथास्थितिवाद ही स्वीकार्य है, बदलाव नहीं। केन्द्र के सभी कार्य अंग्रेजी में ही होते हैं। खानापूर्ति के लिए कहीं-कही अनुवाद जरूर होता है। बहुत-सी सवाल उठाए जा सकते हैं !